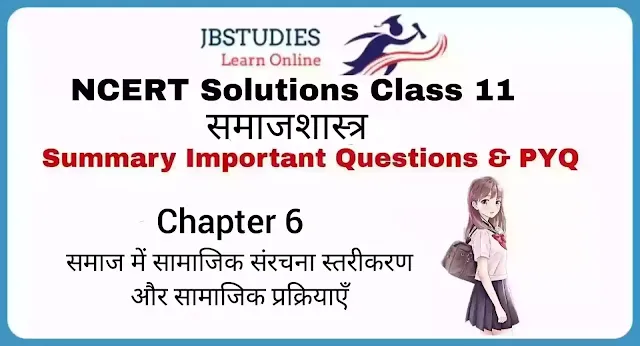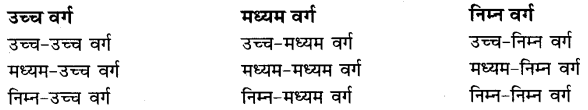NCERT Solutions Class 11 Sociology in Hindi Chapter 6– (समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएँ)
Class 11 (समाजशास्त्र )
अभ्यास के अन्तर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर
पाठ-6 (समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएँ)
प्रश्न 1.
कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में सहयोग के विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।
उत्तर-
कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि इनका संचालन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए भिन्न-भिन्न योग्यताओं वाले व्यक्तियों में सहयोग की आवश्यकता होती है। समाज में श्रम-विभाजन का प्रारंभ इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। श्रम-विभाजन द्वारा विभिन्न व्यक्ति अपने-अपने निर्धारित कार्य करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होते हैं। उदाहरणार्थ-कृषि के क्षेत्र में किसान हल तो चला सकता है परंतु उसे हल के लिए लुहार एवं बढ़ई के सहयोग की आवश्यकता होती है। फसल बोने एवं काटने के समय उसे कृषि श्रमिकों का सहयोग लेना पड़ता है। इस प्रकार के सहयोग के बिना कृषि उत्पादन संभव नहीं है। इसी भॉति, उद्योग भी सहयोग द्वारा ही संचालित होता है। किसी भी उद्योग में काम करने वाले श्रमिक एवं प्रबंधक श्रम-विभाजन के अनुसार अपने-अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करते हैं। यदि किसी एक वर्ग का सहयोग बंद हो जाए तो उत्पादन प्रक्रिया मंद हो सकती है अथवा पूरी तरह से बंद भी हो सकती है। वस्तुतः मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए अन्य लोगों पर आश्रित है। तथा वह इनकी पूर्ति अन्य लोगों के सहयोग द्वारा ही कर सकता है।
प्रश्न 2.
क्या सहयोग हमेशा स्वैच्छिक अथवा बलातु होता है? यदि बलात् है, तो क्या मंजूरी प्राप्त होती है अथवा मानदंडों की शक्ति के कारण सहयोग करना पड़ता है? उदाहरण सहित चर्चा करें।
उत्तर-
सहयोग स्वैच्छिक अथवा बालत् दोनों प्रकार का हो सकता है। श्रम-विभाजन में पाया जाने वाला सहयोग स्वैच्छिक होता है। यदि यह स्वैच्छिक सहयोग न हो तो मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो सकता है। दुख़म जैसे प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों का मत है कि मानव जाति में भूख तथा प्यास जैसी मौलिक संतुष्टि भी सहयोग द्वारा ही संभव है। उन्होंने एकता को समाज का नैतिक बल माना है। तथा इसके आधार पर सहयोग को समझने का प्रयास किया है। श्रम-विभाजन में सहयोग निहित होता है तथा इसीलिए यह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। श्रम-विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। दुर्चीम जैसे समाजशास्त्रियों का मत है कि मनुष्यों की अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सहयोग करना होता है तथा अपने एवं अपनी दुनिया के लिए उत्पादन व पुनरुत्पादन करना पड़ता है। दुर्णीम के विपरीत माक्र्स ने इस तथ्य पर बल दिया है कि ऐसे समाज में, जहाँ वर्ग विद्यमान होते हैं, सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता। इस प्रकार का सहयोग बलात् सहयोग कहलाता है। मार्क्स ने उन उत्पादक शक्तियों, जिन पर मनुष्य को किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता,,को बलात् सहयोग के लिए उत्तरदायी माना है। मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष का सहारा लेना पड़ सकता है। कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करते हैं परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधी को परिभाषित करते हैं। प्रभावशाली समूहों द्वारा बार कई बार जबरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा भी सहयोग लेने का प्रयास किया जाता है। संतुष्टि तथा सृजनात्मकता का भाव जो एक बुनकर या कुम्हार या लुहार को अपने काम से मिलता है। स्वैच्छिक सहयोग का उदाहरण है। दूसरी ओर, एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन में लीवर खींचना या बटन दबाना होता है, आरोपित या बलात् सहयोग का उदाहरण है। इसी भाँति, परिवार के सदस्यों में पाया जाने वाला सहयोग स्वैच्छिक होता है, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में पाया जाने वाला सहयोग आरोपित या बलात् प्रकृति का होता है।
प्रश्न 3.
क्या आप भारतीय समाज से संघर्ष के विभिन्न उदाहरण हुँढ सकते हैं? प्रत्येक उदाहरण में कौन-से कारण थे जिसने संघर्ष को जन्म दिया है? चर्चा कीजिए।।
उत्तर-
भारतीय समाज में संघर्ष के अनेक उदाहरण हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आर्थिक असमानता अर्थात् उत्पादन के साधनों पर असामन नियंत्रण तथा नृजातीयता जैसे अनगिनत स्रोत भारतीय समाज में संघर्ष के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों तथा दंगों के रूप में प्रतिफलित होती है। इसी भाँति, जातिवाद जातीय संघर्षों (जिनमें अधिकांशतः उच्च जातियाँ निम्न जातियों का शोषण करती हैं या उन पर अत्याचार करती हैं) तथा क्षेत्रवाद विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों में होने वाले संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। यह संघर्ष जल के बँटवारे अथवा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण आदि के आधार पर विकसित होता है। क्षेत्रवाद ऐसी भावनाओं को जन्म देता है जो अन्य क्षेत्रों के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली होती हैं। उदाहरणार्थ-कई बार महाराष्ट्र या असम में अन्य प्रदेशों के लोगों को नौकरी देने का प्रबल विरोध क्षेत्रवाद की भावना के आधार पर ही किया जाता है। असम में अनेक गैर-असमी लोगों की हिंसा इसी प्रकार के संघर्ष का परिणाम है।
प्रश्न 4.
संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाता है इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए।
उत्तर-
सहयोग एवं संघर्ष जीवन के दो अभिन्न पहलू माने जाते हैं। दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य हैं परंतु संघर्ष का सहयोग के अंतर्गत होना समाज के अस्तित्व के लिए उपयोगी माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक समाज संघर्ष को कम-से-कम करने का प्रयास करता है। यह दूसरी बात है कि संघर्ष के लिए उत्तरदायी कारण जब तक समाज में विद्यमान हैं तब तक संघर्ष को कम करना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ-जब तक अमीर एवं गरीब में अत्यधिक अंतराल, विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक आर्थिक असमता अथवा विकास, विभिन्न समूहों में राष्ट्र के स्थान पर अपने ही समूह के प्रति वफादारी होगी, तब तक समाज में संघर्ष कम नहीं हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले उन सब कारणों का पता लगाया जाए जो संघर्ष के लिए उत्तरदायी हैं। इन सब कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाए तथा विवादित मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने का भरसक प्रयास किया जाए। सरकार किसी भी संप्रदाय, प्रदेश अथवा जाति विशेष के प्रति राजनीतिक कारणों के किए जाने वाले भेदभाव की नीति न अपनाए तो संघर्ष को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।
सांप्रदायिकता के आधार पर होने वाले अधिकांश संघर्ष छोटी-छोटी बातों, भ्रम तथा अफवाहों पर आधरित होते हैं। कई बार तो शरारती तत्त्व अपनी या अपने राजनीतिक दल की स्वार्थ सिद्धि हेतु भी। इस प्रकार के संघर्षों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे तत्त्वों पर निरंतर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। तथा यह कार्य सरकार तभी कर सकती है जबकि सरकार का संचालन करने वाले सभी संबंधित राजनेता, अधिकारी तथा प्रशासक आदि स्वयं लौकिक राज्य के मूल्यों के प्रति समर्पित हों। निर्धनता, बेरोजगारी जैसी समस्याएँ भी संषर्घ का कारण होती हैं तथा इन पर भी अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। संसाधनों का वितरण भी इस ढंग से किया जाना आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों में किसी प्रकार का रोष या वंचना की भावना विकसित न हो।
वस्तुत: संघर्ष पर नियंत्रण करना अथवा इसे कम करना अत्यंत कठिन कार्य है तथा कोई भी समाज इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। माक्र्सवादी विद्वानों का तो यह मत है कि समाज से संघर्ष समाप्त करना तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति द्वारा साम्यवाद की स्थापना न हो। उनका यह तर्क ऐतिहासिक प्रमाणों की दृष्टि से सही साबित नहीं हुआ है। तथा सोवियत संघ के विघटन तथा पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के परिणमस्वरूप यह मत और भी अधिक कमजोर हो गया है।
प्रश्न 5.
ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्या यह संभव है? अगर नहीं तो क्यों?
उत्तर-
आज प्रतिस्पर्धा को विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक माना जाता है। इसीलिए समकालीन समाजों में प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत के रूप में विद्यमान है। पूँजीवादी समाजों में तो प्रतिस्पर्धा एक सशक्त विचाराधारी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि परंपरागत समाजों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान थे तथा एक जैसे कार्यों में लगे हुए थे। दुर्णीम के अनुसार, इस प्रकार के समाजों में ‘यांत्रिक एकता’ पायी जाती है। अनेक मार्क्सवादी विद्वान् संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा विहीन समाज की कल्पना को नकराते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि सभी ज्ञात समाजों में किसी-न-किसी रूप में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा विद्यमान थी। यदि देखें तो सरलतॆम समाजों में भी प्रतिस्पर्धा किसी-न-किसी रूप में प्रचलित थी। उदाहरणार्थ-जनजातियों में जीवनसाथी के चयन हेतु परीक्षा विवाहे, जिसमें विवाह के इच्छुक लड़कों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अथवा प्राचीन समाजों में होने वाले खेलकूल मुकाबलों में विजेता को पुरस्कृत करना आदि प्रतिस्पर्धा के ही उदाहरण हैं। स्वाभाविक वृत्ति के रूप में भी प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इसलिए ‘विजेता तथा पराजित’ जैसे शब्दों का व्यक्ति अथवा समूह के लिए प्रचलन प्रतिस्पर्धा से ही संबंधित रहा है। इतना अवश्य है कि परंपरागत समाज प्रतिस्पर्धा को उस सीमा तक नहीं होने देते थे जहाँ यह संघर्ष का कारण बन जाए। जनजातियों में परंपरागत रूप से सबसे बड़े शिकारी या बहादुर का मुखिया होना भी इस बात का प्रतीक है कि उसके इस गुण का चयन किसी-न-किसी प्रतिस्पर्धा पर ही आधारित रहा होगा। अपनी भूख, प्यास जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी विभिन्न समूहों में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के उदाहरण मिलते हैं, इसीलिए पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा-विहीन समाज की कल्पना करना संभव नहीं है।
प्रश्न 6.
अपने माता-पिता, बड़े बुजुर्गों तथा उनके समकालीन व्यक्तियों से चर्चा कीजिए कि क्या आधुनिक समाज सही मायनों में प्रतिस्पर्धात्मक है अथक पहले की अपेक्षा संघर्षों से भरा है और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे समझाएँगे?
उत्तर-
निश्चित रूप से आधुनिक समाज प्रतिस्पर्धात्मक है तथा पहले से कहीं अधिक संघर्षों से भरा है। यदि हम अपने माता-पिता अथवा बड़े बुजुर्गों से बात करें तो इस तथ्य की पुष्टि सरलता से हो जाती है। आधुनिक युग के विपरीत पहले हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता था। समाज में हितों में टकराव न्यूनतम था तथा संघर्ष को यथासंभव विकसित होने से पहले ही रोकने का प्रयास किया जाता था। व्यक्तियों के समूह अपनी जंगली जानवरों से रक्षा तथा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में परस्पर सहयोग करते थे तथा जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध होता था उसे मिल-बाँटकर खा लेते थे। विभिन्न समूहों में सेवाओं अथवा वस्तुओं का विनिमय पाया जाता था जो प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को न्यूनतम कर देता था। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यदि इस स्थिति को देखा जाए तो व्यक्ति अपनी प्रस्थिति के बारे में यह सोचकर संतुष्ट हो जाता था कि शायद भगवान की ही ऐसी इच्छा है। वह अपनी वंचना अथवा उपलब्धि को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मानकर ही संतोष कर लेता था। इतना अवश्य है कि तब भी विभिन्न समूहों में किसी-न-किसी बात को लेकर संघर्ष होते रहते थे। आधुनिक समाजों में व्यापार के विस्तार, श्रम-विभाजन, विशेषीकरण तथा बढ़ती उत्पादकता ने व्यक्तिवाद एवं प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक बढ़ा दिया है। उदाहरणार्थ-आधुनिक समाजों में प्रतिस्पर्धा ही यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्यकुशल फर्म ही बची रहेगी। प्रतिस्पर्धा ही यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र ही किसी प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला ले पाएगा और फिर बेहतरीन रोजगार भी प्राप्त कर सकेगा। प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिस्पर्धा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति न होकर पूँजीवाद के जन्म के साथ ही प्रबल इच्छा के रूप में फली-फूली है। संसाधनों की कमी तथा प्रत्येक समूह द्वारा संसाधनों पर कब्जा करने का प्रयास संघर्ष को विकसित करता है। इसीलिए आज सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष बढ़ गए हैं। वर्ग अथवा जाति, जनजाति अथवा लिंग, नृजातीयता अथवा धार्मिक समुदायों में होने वाले संघर्ष आज की प्रस्थिति के द्योतक हैं।
आधुनिक समाजों में संघर्ष की वृद्धि का एक कारण सामाजिक परिवर्तन तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुविधा-वंचित तथा भेदभाव का सामना कर रहे समूहों द्वारा हक जताना तथा सामाजिक संरचना को परिवर्तित करना भी है। अत्यधिक संघर्ष को व्याधिको माना जाता है जो कि विकास को अवरुद्ध करती है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा को स्वाभाविक प्रक्रियाएँ नहीं मानता है। यह उन्हें सामाजिक संरचना से जोड़कर देखने का प्रयास करता है तथा सामाजिक विकास से भी जोड़ता है।
क्रियाकलाप आधारित प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
अपने बड़े-बुजुर्गों( दादा-नाना) अथवा उनकी पीढी के अन्य लोगों से बातचीत कर यह पता कीजिए कि परिवारों/विद्यालयों में किस प्रकार का परिवर्तन आया है तथा किन-किन पक्षों में वे आज भी वैसे ही हैं। (क्रियाकलाप 1)
उत्तर-
अपने बड़े-बुजुर्गों (दादा/नाना) अथवा उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों से बातचीत कर यह सरलता से पता लगाया जा सकता है कि परिवारों एवं विद्यालयों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। पहले परिवार समाजवादी विचारधारा पर आधारित थे तथा परिवारवाद के कारण न तो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विकसित होती थी और न ही संबंधों में औपचारिकता आने का डर रहता था। परिवार के सभी सदस्य अपने हितों की तुलना में अपने परिवार के हित को प्राथमिकता देते थे। सभी का यही प्रयास रहता था कि किसी भी सदस्य में असुरक्षा की भावना विकसित न होने पाए। परिवार का वयोवृद्ध सदस्य न केवल बच्चों के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता था अपितु सभी सदस्य उसके नियंत्रण में भी रहते थे। वही परिवार के सभी मामलों के बारे में निर्णय लेता था तथा कोई भी सदस्य उसके निर्देश की अवहेलना नहीं करता था। वह भी सभी सदस्यों का ध्यान रखता था तथा उनको उनकी योग्यता, आयु एवं लिंग के आधार पर कार्यों को सौंपता था। इसीलिए परंपरागत रूप में परिवार तथा घर सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते रहे हैं जहाँ सहयोग, प्रभुत्व, प्रक्रिया तथा परार्थवाद मनुष्य के आचरण के प्रेरणात्मक सिद्धांत थे।
आधुनिक युग में परिवार का यह रूप परिवर्तित हो गया है। परिवार के सदस्यों में औपचारिकता आ गई है तथा सदस्यों पर इसका नियंत्रण शिथिल हो गया है। परिवार के अधिकांश कार्य अन्य संस्थाओं ने ले लिए हैं जिससे इसका महत्त्व भी पहले से कम हो गया है। परिवार के आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक सभी प्रकार के कार्यों में परिवर्तन हुआ है। सहयोग एवं परार्थवाद को भी अब नारीवादी विश्लेषकों द्वारा चुनौती दी जाने लगी है। इन विद्वानों तथा अमर्त्य सेन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चूंकि संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता; अतः यह देखा गया है। कि मध्यम वर्ग में महिलाएँ संघर्षों में समायोजन तथा सहयोग पाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाती रही हैं। उनकी यह सतत प्रयास रहता है कि संघर्षों को आपसी सहयोग द्वारा निपटाया जाए तथा साथ ही संघर्ष की विचलित व्यवहार के रूप में देखा जाए।
परिवार की भाँति विद्यालय का रूप भी अब पहले जैसा नहीं रहा है। न तो विद्यालयों में पढ़ने वाले पहले जैसे शिक्षार्थी हैं और न ही पढ़ाने वाले शिक्षक। अनुशासन की दृष्टि से आज विद्यालयों का माहौल पहले से कहीं खराब है। शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले बहुत कम लोग शिक्षा हेतु विद्यालयों में आते थे, जबकि अब विद्यालयों में प्रवेश लेना ही कठिन है। शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात अत्यधिक होने के कारण किसी भी विद्यालय में शिक्षक अपने शिष्यों को न तो पूरी तरह से जानता है और न ही उनका उचित विकास कर पाता है। विद्यालयों में भी नौकरशाही संगठन जैसी विशेषताएँ विकसित हो गई हैं तथा यह सर्वांगीण विकास का अभिकरण न होकर मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनकर रह गया है। आज शिक्षक अपना ध्यान केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही केंद्रित करते हैं तथा बच्चों की रुचियों को विकसित करने की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं।
प्रश्न 2.
पुराने चलचित्रों/धारावाहिकों/उपन्यासों में परिवारों के प्रस्तुतीकरण की तुलना समकालीन प्रस्तुतियों से कीजिए। (क्रियाकलाप 1)
उत्तर-
पुराने चलचित्रों/धारावाहिकों/उपन्यासों में परिवारों का प्रस्तुतीकरण संयुक्त परिवार के रूप में किया जाता था जिसमें सदस्यों के एक-दूसरे के प्रति स्नेह एवं त्याग को दिखाया जाता था। प्रत्येक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक भाई, एक पति, एक पिता या दादा अथवा देश के नागरिक के रूप में करते हुए दर्शाया जाता था। परिवार में बड़े-बूढ़ों के सम्मान तथा श्रम-विभाजन की एक आदर्श व्यवस्था पर आधारित एक इकाई के रूप में इसका प्रस्तुतीकरण एक सामान्य बात थी। आधुनिक चलचित्रों/धारावाहिकों/उपन्यासों में परिवार का जो रूप प्रस्तुत किया जाता है वह पहले से पूरी तरह से भिन्न है। आज इनमें उच्च वर्ग के परिवारों को दर्शाया जाता है जिनमें महिलाओं एव लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता होती है तथा वे अपनी परंपरागत भूमिका से भिन्न भूमिका निभाती हुई दर्शाई जाती हैं। समाज की मान्यताओं के आदर्शों को तोड़ना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं है। अधिकांश परिवारों में बच्चों को बिगड़े हुए, माता-पिता को परस्पर या बच्चों से लड़ते-झगड़ते, भाइयों की संपत्ति पर अधिकार को लेकर एक-दूसरे पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हुए और स्त्रियों को एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हुए तथा विवाह-पूर्व एवं विवाहेतर संबंधों में लिप्त दिखाया जाना सामान्य बात है। टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले अनेक धारावाहिकों में कुछ चरित्र ऐसे दर्शाए गए हैं जो तीन-चार बार विवाह करते हैं, विवाहेतर संबंधों को प्राथमिकता देते हैं तथा अपने पैसे के बल पर अपने प्रतियोगी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने में संकोच नहीं करते हैं। स्त्रियों को भी एक-दूसरे के प्रति विद्वेष करते या षड्यंत्र रचते हुए दर्शाया जाता है। सास-बहू के संबंध या तो अत्यधिक मुधर या बहुधा संघर्षमयी दर्शाए जाते हैं। अधिकांश अमीर परिवारों का प्रस्तुतीकरण इस रूप में किया जाता है कि माता-पिता को एक-दूसरे का ध्यान रखने तथा अपने बच्चों को देखने का समय ही नहीं होता।
प्रश्न 3.
क्या आप अपने परिवार में सामाजिक आचरण के प्रतिमानों (पैटर्स) और नियमितताओं | को समझते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या आप अपने परिवार की संरचना का वर्णन कर सकते (क्रियाकलाप 1)
उत्तर-
परिवार में आचरण के कुछ मानक स्तर, विवाह के तौर-तरीके, संबंधों के अर्थ, पारस्परिक उम्मीदें तथा उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला माना गया है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा ही शिशु को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है अर्थात् उसे सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों एवं आदर्शों से परिचय कराता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वैसे-वैसे परिवार के सदस्य उसे बोलना, चलना, बड़ों को नमस्ते करना, लिंगानुसार कपड़े पहनना आदि सिखाते हैं। समाजीकरण की यह प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर नियमित रूप से होती रहती है। परिवार की अपनी एक संरचना होती है जिमसें प्रत्येक सदस्य का एक निश्चित स्थान (प्रस्थिति) एवं भूमिका होती है। वह अपनी निर्धारित प्रस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करते हुए परिवार को बनाए रखने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप पुरुषों एवं महिलाओं की प्रस्थिति एवं क्रम निर्धारित होता है। विवाहोपरांत सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप लड़की लड़के के परिवार में चली जाती है, जबकि लड़के के विवाह के समय दूसरे परिवार की लड़की लड़के के परिवार की सदस्य बन जाती है। इसके साथ ही, परिवार में वृद्ध सदस्यों की मृत्यु एवं नए सदस्यों का प्रवेश निरंतर होता रहता है। इसीलिए परिवार निरंतर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में परिवर्तन नहीं होता, अपितु परिवर्तन के बावजूद परिवार की संरचना में निरंतरता पायी जाती है।
प्रश्न 4.
विद्यालय को एक संरचना के रूप में आपके शिक्षक कैसे लेते हैं। इस पर उनसे विचार-विमर्श कीजिए। क्या छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को इस संरचना को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष रूप से काम करना पड़ता है? (क्रियाकलाप 1)
उत्तर-
परिवार की भाँति विद्यालय की भी एक निश्चित संरचना होती है। विद्यालय का प्रबंधतंत्र, प्राचार्य/प्राचार्या, शिक्षकगण, गैर-शिक्षक कर्मचारी तथा छात्र-छात्राएँ इस संरचना के महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। वे सभी प्रकार निर्धारित भूमिका निभाते हुए विद्यालय की संरचना को बनाए रखते हैं। विद्यालय में कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप वर्षों से दोहराए जाते हैं जो आगे जाकर संस्थाएँ बन जाते हैं; उदाहणार्थ-विद्यालय में दाखिले के तरीके, प्रात:कालीन सभा और कहीं-कहीं विद्यालयी गीत, आचरण संबंधी नियम, वार्षिकोत्सव इत्यादि। विद्यालय से पुराने विद्यार्थियों का चले जाना तथा उनके स्थान पर नए विद्यार्थियों का प्रवेश निरंतर होता रहता है। इसी भाँति, शिक्षक निर्धारित आयु पर सेवानिवृत्ति होते हैं तथा उनका स्थान नए शिक्षक ले लेते हैं। इस भॉति यह संस्था निरंतर चलती रहती है।
विद्यालय की संरचना बनाए रखने में छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें उनकी भूमिका कहा जाता है। प्रत्येक को अपनी भूमिका का निर्वहन उचित ढंग से करना पड़ता है। छात्रों से आशा की जाती है कि वे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखें, अपनी कक्षाओं में मन लगाकर पढ़े, खाली घंटे में खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में भाग लें तथा अपनी समस्याओं के समाधान में शिक्षकों का सहयोग लें। शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे छात्रों को उचित शिक्षा एवं ज्ञान दें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे विद्यालय में ऐसा व्यवहार करें जो छात्रों के लिए अनुकरणीय हो क्योंकि अधिकांश छात्र अपने शिक्षकों को ही अपना आदर्श मानते हैं। कई बार शिक्षकों की कही गई बातों का छात्रों पर प्रभाव उनके माता-पिता द्वारा कही गई बातों से भी अधिक पड़ता है। विद्यालय के अन्य कर्मचारियों से भी अपनी प्रस्थिति के अनुकूल भूमिका निष्पादन की आशा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति लिपिक है तो वह उस निर्धारित कार्य को समय पर पूरा करे जो उसे दिया गया है। इसी भाँति, यदि कोई चपरासी है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह कक्षाओं को साफ-सुथरा रखे, समय पर घंटा लगाए तथा अन्य जो कार्य उसे सौंपा जाता है उसका ठीक प्रकार से निर्वहन करे।
प्रश्न 5.
क्या आप अपने विद्यालय अथवा परिवार में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सोच सकते | हैं? क्या इन परिवर्तनों का विरोध हुआ? किसने इनका विरोध किया और क्यों? (क्रियाकलाप 1)
उत्तर-
आधुनिक युग में विद्यालयों अथवा परिवारों में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। उदाहरणार्थ-विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन समिति का गठन किया जाता है। ही समिति बाहर घूम रहे छात्रों की जाँच कर उन्हें कक्षाओं में बैठने के लिए कहती है। न मानने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है। आजकल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनेक छात्र-छात्राएँ मोबाइल फोन लेकर आने लगे हैं। उन पर बजने वाली घंटी न केवल कक्षाओं का माहौल बिगाड़ती है अपितु अनुशासन की अनेक समस्याएँ भी विकसित हो जाती हैं। इसलिए अनेक विद्यालय एवं महाविद्यालय मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रतिबंध का छात्र-छात्राएँ इस आधार पर विरोध करते हैं कि मोबाइल फोन तो उनके माता-पिता ने सुरक्षा की दृष्टि से देख रखा है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर वे उनसे संपर्क स्थापित कर सकें। उनके माता-पिता भी यही तर्क देते हैं। इस विरोध के कारण छात्रों को हड़ताल तक भी करनी पड़ी तथा शिक्षकों एवं प्रशासकों से अभद्र व्यवहार की घटनाएँ भी सामने आईं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों में; मोबाइल फोन में लगे कैमरे में न केवल अश्लील दृश्य कैद किए गए हैं, अपितु साथियों को उन्हें एस०एम०एस० के माध्यम से भेजकर उनका प्रसार भी किया गया है। इसी आधार पर विद्यालय इनके प्रयोग को विद्यालय परिसर में प्रतिबंधित करने का तर्क देते हैं।
प्रश्न 6.
ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए जो दोनों स्थितियों को प्रकट करते हों-किस प्रकार मनुष्य सामाजिक संरचना से बाध्य होता है तथा जहाँ व्यक्ति सामाजिक संरचना की अवहेलना करता है और उसे बदल देता है। | (क्रियाकलाप 2)
उत्तर-
प्रत्येक समाज की संरचना अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाती है। दुम जैसे समाजशास्त्रियों का कहना है कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक है; इसमें ‘दृढ़ता’ अथवा ‘कठोरता है जो भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान होती है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कमरे में खड़ा है जहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। कमरे की संरचना उसकी संभावित क्रियाओं को बाध्य करती है। उदाहरणार्थ-दीवारों तथा दरवाजों की स्थिति प्रवेश तथा निकास के रास्तों को दर्शाती है। इसी भॉति, परिवार की सामाजिक संरचना प्रत्येक सदस्य के अनचाहे व्यवहार पर अंकुश लगाती है। परिवार के सदस्य न चाहते हुए भी पारिवारिक मान्यताओं का पालन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अत्यधिक अंकुश सदस्यों को उन मान्यताओं को तोड़ने या पारिवारिक संरचना की अवहेलना करने पर विवश कर देता है। परंपरागत रूप से लड़के-लड़कियों हेतु जीवनसाथी का चयन परिवार के वृद्ध सदस्यों अथवा उनके माता-पिता द्वारा किया जाता है। आज लड़के-लड़कियाँ स्वयं अपने जीवनसाथी का चयन करने लगे हैं। यदि परिवार के वृद्ध सदस्य या माता-पिता उनकी इस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं तो वे परिवार से अलग होकर अपना एकल परिवार बनाने की धमकी देकर परिवार के इस नियम की अवहेलना भी करने लगते हैं।
प्रश्न 7.
अपने प्रतिदिन के जीवन में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष के उदाहरण हूँढिए। (क्रियाकलाप 3)
उत्तर-
हममें से प्रत्येक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य लोगों पर आश्रित है। अन्य लोगों का अप्रत्यक्ष सहयोग ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति को संभव बनाता है। उदाहरणार्थ-कपड़ों के लिए हम कपड़े के दुकानदार पर निर्भर हैं, इसकी सिलाई के लिए दर्जी पर, इसकी धुलाई के लिए साबुन या सर्फ बनाने वाली कंपनी पर तथा कपड़ों को इस्त्री करने के लिए धोबी या बिजली की प्रेस बनाने वाली कंपनी तथा बिजली पर। सहयोग की ही भाँति हमें निरन्तर प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती है। कॉलेज में प्रवेश हेतु अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अथवा नौकरी प्राप्त करने के लिए भी हमें अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। खेलकूद के समय भी प्रत्येक खिलाड़ी का यह प्रयास रहता है कि वह अन्य की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि राज्य स्तर पर होने वाली खेल प्रतिस्पर्धाओं में उसकी टीम के सदस्य के रूप में चयन हो सके। कारखाने अथवा अन्य किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक तथा मजदूर या कर्मचारी अपने प्रतिदिन के कार्यों में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करता है। वास्तविकता यह है कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते।
प्रश्न 8.
क्या विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएँ अपने आपको संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं? क्या वे पुरुषों के उत्तराधिकार के मानदंड से सहयोग इसलिए करती हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो भाइयों के प्रेम से वंचित हो जाएँगी? (क्रियाकलाप 4)
उत्तर-
यह सही है कि विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएँ अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं। उनका यह सहयोग ‘स्वैच्छिक न होकर ‘बाध्य होता है। अपने जन्म के परिवार में संपत्ति पर महिला का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे का विश्लेषण करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। महिलाएँ संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपने जन्म के परिवार की संपत्ति पर दावा नहीं करतीं, क्योंकि वे डरती हैं कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी या भाभियाँ उनसे घृणा करने लगेंगी और परिणामस्वरूप अपने पिता के घर उनका आना-जाना बंद हो जाएगा। लीला दुबे ने अपने अध्ययन में यह पाया कि 41.7 प्रतिशत महिलाएँ इसी डर के कारण जन्म के परिवार (नेटल परिवार) से संपत्ति में अपने हिस्से की माँग नहीं करती हैं। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में महिलाएँ संपत्ति से अपना हिस्सा लेने से इनकार करने पर भी अपने जन्म के परिवार की उन्नति में सहायक होने और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा रखती हैं। यह ऐसे सहयोगात्मक व्यवहार का उदाहरण है जो समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है। जब तक ऐसे संघर्षों की खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा उन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक यह छवि बनी रहती है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। प्रकार्यवादी समाजशास्त्री ऐसी परिस्थिति को व्यक्त करने हेतु ‘व्यवस्थापन’ शब्द का भी प्रयोग करते हैं।
प्रश्न 9.
कुछ अन्य सामाजिक व्यवहारों के बारे में सोचिए जो सहयोगात्मक दिखाई देते हों परंतु समाज के गहरे संघर्षों को अपने अंदर छिपाए हों। (क्रियाकलाप 5)
उत्तर-
महिलाओं द्वारा अपने जन्म के परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से की माँग न करने जैसे अनेक अन्य उदाहरण भी हैं जो सहयोगात्मक दिखाई देते हैं परंतु उनमें समाज के गहरे संघर्ष का आभास होता है। हम एक ऐसे परिवार का उदाहरण ले सकते हैं जिसमें दो भाई हैं जिनमें संपत्ति को लेकर मतभेद है तथा वे एक-दूसरे से अलग होना चाहते हैं। इस बात के डर से कि कहीं पिता उन दोनों को पैतृक संपत्ति से बेदखल न कर दे, वे पिता के जीते जी संपत्ति के बँटवारे की बात ही नहीं करते हैं। एक-दूसरे को न चाहते हुए अथवा गहरे मतभेद होते हुए भी वे एक ही परिवार के सदस्य के रूप में रहने के लिए तब तक विवश हो जाते हैं जब तक कि उनका पिता जीवित है। पिता की मृत्यु के पश्चात् संपत्ति बँटवारे को लेकर वे आपस में कोई समझौता कर लेते हैं अथवा बहुधा उनका यह छिपा हुआ संघर्ष सार्वजनिक भी हो सकता है। कई बार तो बँटवारे संबंधी संघर्ष इतना गहरा होता है कि वाद न्यायालय तक पहुँच जाता है।
प्रश्न 10.
अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के सरकार के निर्णय के पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए विभिन्न तर्को को एकत्रित कीजिए। (क्रियाकलाप 6)
उत्तर-
शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हिन्दू एवं मुस्लिम जातियों का पता लगाने हेतु 1953 ई० में एक पिछड़ा वर्ग कमीशन’ बनाया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। कमीशन ने चार आधारों पर पिछड़ेपन का पता लगाने का प्रयास किया–जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा व्यापार, वाणिज्य व उद्योग के क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। 1977 ई० में जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने पर अपने । घोषणा-पत्र के अनुरूप ‘मण्डल कमीशन’ नियुक्त किया। इस बहुचर्चित कमीशन ने देश की 52 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी सेवाओं व शिक्षा संस्थाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया जिसे अन्ततः श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रीत्व “काल में काफी विरोध के बावजूद स्वीकार कर लिया गया। अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थाने हेतु भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के अधीन 13 जनवरी, 1992 ई० को ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य इन वर्गों के कल्याण के लिए आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना था।
अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया आरक्षण प्रारंभ से ही वाद-विवाद का विषय रहा है। इनके आरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि इन वर्गों का सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान इसी के द्वारा सम्भव है। इनके आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि आर्थिक पिछड़ेपन का आधार जाति नहीं हो सकता। या तो सभी जातियों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिले या इस आरक्षण को रद्द कर दिया जाए। साथ ही, अन्य पिछड़े वर्गों में ‘क्रीमी लेयर’ का मुद्दा भी विवादास्पद रहा है। इससे यह अभिप्राय है कि अन्य पिछड़े वर्गों में जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
अभी हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इस आरक्षण का लाभ उठाने वाली जातियों की जनंसख्या का पता नहीं है। 1931 ई० में जनगणना में भारत में जाति के आधार पर भी गणना की गई थी। आरक्षण में इसी को आधार बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि 1931 ई० की जनगणना को आरक्षण को आधार बनाया जाना अनुचित है। अभी स्थिति यह है कि शिक्षा संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण न्यायालय के आदेश के कारण स्थगित है तथा इस मुद्दे पर न्यायालय का एक बड़ा बैंच विचार-विमर्श कर रहा है।
प्रश्न 11.
विद्यालय में ड्रॉप आउट की दर, विशेषकर प्राइमरी विद्यालयों में, पर जानकारी हासिल कीजिए। (क्रियाकलाप 6)
उत्तर-
विद्यालयों में ‘ड्रॉप आउट’ की दर से अभिप्राय उस अनुपात से है जिसमें प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएँ अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं अर्थात् वे प्रवेश तो लेते हैं परंतु पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ देते हैं। इस प्रकार के ‘ड्रॉप आउट’ पर अनेक अध्ययन हुए हैं। ब्रजराज चौहान द्वारा किए गए। अध्ययन से पता चलता है कि ड्रॉप आउट’ की दर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में अधिक है। पहले तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का शिक्षा संस्थाओं में नामांकन ही अपर्याप्त है तथा दूसरे, जो नामांकन में सफल भी हो जाते हैं उनमें ‘ड्रॉप आउट’ की दर भी अधिक है। इसका कारण इन जातियों की परंपरागत स्थिति एवं व्यवसाय है। अधिकांश निर्धन परिवारों में बच्चे को तनिक बड़ा होते ही रोजी कमाने के काम पर लगा दिया जाता है। पढ़ाई की तुलना में बच्चे का परिवार की आमदनी का स्रोत बनना अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। बहुत-से माता-पिता पढ़ाई पर होने वाले व्यय को भी वहन नहीं कर पाते। विशिष्ट व्यावसायिक संस्थानों में यह बात और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। ‘ड्रॉप आउट’ की यह दर 10 से 25 प्रतिशत तक हो सकती है। जैसे-जैसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है, वैसे-वैसे ‘ड्रॉप आउट’ की यह दर कम होती जा रही है।
प्रश्न 12.
“प्रतिस्पर्धा समाज के लिए सकारात्मक तथा आवश्यक है।” इस विषय पर वाद-विवाद का आयोजन कीजिए। (क्रियाकलाप 7)
उत्तर-
क्या आधुनिक समाजों में प्रतिस्पर्धा सकारात्मक एवं आवश्यक है? यह एक वाद-विवाद का प्रश्न है। एक तरफ इसका पक्ष लेने वाले लोगों का कहना है कि आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रतिस्पर्धा के संगठनात्मक दृष्टि से अच्छे परिणाम होते हैं। क्योंकि इससे प्रत्येक व्यवसाय में अच्छे लोगों को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है। यदि समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर प्रतिस्पर्धा होती है तो यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा में लगे व्यक्ति अन्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे उनका दृष्टिकोण विस्तृत बनता है, बोध शक्ति बढ़ती है और सहानुभूति गहरी होती है। ये सभी बातें व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहन देती हैं। इससे समाज में प्रगति होती है तथा सामाजिक एकता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। यह व्यक्ति, समूह एवं समाज की दृष्टि से प्रकार्यात्मक है और इसी दृष्टि से यह एक संगठनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। प्रतिस्पर्धा कार्यों को अच्छी प्रकार से करने की प्रेरणा देती है, यह महत्त्वाकांक्षाओं में वृद्धि करती है तथा प्रतिद्वंद्वी की चुनौती को स्वीकार कर अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्रदान करती है।
प्रतिस्पर्धा की सकारात्मक भूमिका एवं आवश्यकता के विपक्ष में जो दिए जाते हैं उनमें बहुधा प्रतिस्पर्धा का कटु रूप धारण कर लेना प्रमुख है। प्रतियोगी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी नियमों को तोड़कर अवैधानिक साधन अपनाने लगते हैं। कई बार कटुता इतनी अधिक हो जाती है कि प्रतिद्वद्वियों में संघर्ष तक हो जाता है। इसी दृष्टि से इसके असहयोगी परिणामी की विवेचना की जाती है। गिलिन तथा गिलिन जैसे समाजशास्त्रियों के मतानुसार प्रतिस्पर्धा सामाजिक विघटन के लिए भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी है।
जे०एस० मिल जैसे उदारवादियों ने भी प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को अधिकतर नुकसानदायक माना है। उनका तर्क है कि प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष की आवश्यकताओं को थोपने से समाज में व्यक्तिवाद का तीव्रता से विस्तार होता है।
इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा आविष्कारों को प्रोत्साहन देती है और कई बार व्यक्ति उन आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन से अनुकूलन नहीं रख पाते। ऐसी नवीन परिस्थिति में सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि इसमें असामंजस्य की स्थिति विकसित हो जाती है। सामाजिक एकता की बजाय सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन देकर यह अपनी असहयोगी भूमिका निभाती है। साथ ही, अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा में घृणा और हिंसा की भावना आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा हिंसा तथा संघर्ष में भी बदल जाती है और समाज, समूह तथा व्यक्ति के लिए विघटनकारी हो जाती है।
प्रश्न 13.
प्रतिस्पर्धा का विभिन्न विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस विषय पर अपने स्कूल के अनुभवों के आधार पर निबंध लिखिए। (क्रियाकलाप 7)
उत्तर-
आधुनिक युग में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। यह प्रतिस्पर्धा केवल शैक्षिक दृष्टि से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं होती, अपितु विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी इसे स्पष्टतः देखा जा सकता है। खेल के मैदान में प्रत्येक छात्र एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तथा इसलिए अपने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु विद्यालय के अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा करता है। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु अनेक छात्र प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उन्हें अपने प्रतिस्पर्धा से आगे निकलते हेतु अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं कई बार छात्र यह चाहता है कि वह अपने नगर के सभी विद्यालयों के छात्रों से आगे निकले तथा प्रथम स्थान प्राप्त करे। इसके लिए वह परोक्ष रूप से अन्य विद्यालयों के उन छात्रों से भी प्रतिस्पर्धा करता है जिन्हें वह जानता तक नहीं। यह सोचकर कि अपने या अन्य किसी विद्यालय का छात्र उससे अधिक अंक प्राप्त न कर ले, वह दिन-रात एक करके अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा से बोध शक्ति बढ़ती है। विद्यालय के छात्रों पर प्रतिस्पर्धा का नकारात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है। कुछ प्रतियोगी छात्र यह मान लेते हैं। कि वे अमुक छात्र से आगे नहीं निकल सकते। इससे वे हतोत्साहित होते हैं तथा उतना कठिन परिश्रम नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए।
प्रश्न 14.
वे अवसर कौन-से हैं जिनमें हमारे समाज में एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है? (क्रियाकलाप 8)
उत्तर-
आधुनिक युग में सभी स्तरों पर व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश के उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है। पहले कभी विद्यालयों में छह वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था तथा इसके लिए उन्हें या उनके माता-पिता को किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं देना पड़ता था। अब सभी जानते हैं कि अंग्रेजी माध्यम के अच्छे विद्यालयों में प्रवेश की न्यूनतम आयु चार वर्ष से अधिक होती है तथा प्रवेश एल०के०जी० में होता है। प्रथम कक्षा में बच्चा तब प्रवेश करता है जब उसकी आयु छह वर्ष की हो जाती है। अनेक ‘प्ले स्कूल’ एवं ‘नर्सरी स्कूल बच्चों को कम आयु में प्रवेश देकर उनकी योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे विद्यालयों का उद्देश्य बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश हेतु योग्य बनाना है अर्थात् उसे इस लायक बनाना है कि वह अन्य उसी प्रकार के विद्यालयों के बच्चों से प्रवेश के समय अच्छा प्रदर्शन कर सके तथा उसका प्रवेश हो सके। यदि बच्चे का प्रवेश हो जाता है तो कम-से-कम इंटरमीडिएट कक्षा तक उसके माता-पिता उसकी शिक्षा के बारे में निश्चिन्त हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा की इस पहली सीढ़ी को पार करने वाले बच्चे अन्य बच्चों से कहीं आगे निकलने हेतु पुनः प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०ए०, बी-एस०सी०, बी० कॉम आदि में प्रवेश लेने के लिए उन्हें पुनः अन्य बच्चों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यदि प्रवेश प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है तो वही बच्चे प्रवेश पाते हैं जिनका क्रम मैरिट में ऊँचा होता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने हेतु भी प्रतिस्पर्धा से ही गुजरना पड़ता है। इस प्रकार, आधुनिक युग में जीक्न के प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति को किसी-न-किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अभी हमारे देश में ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं हैं कि बच्चा नर्सरी में प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रवेश ले ले तथा वहीं से डॉक्टर या इंजीनियर बनकर निकले। इंग्लैण्ड जैसे देश में बच्चों को इस प्रकार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका में प्रत्येक स्तर पर प्रवेश हेतु बच्चों को अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यही व्यवस्था भारतीय शिक्षा पद्धति की है।
प्रश्न 15.
आज विश्व में वे कौन-से विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं जो विद्यमान हैं? (क्रियाकलाप 9)
उत्तर-
आज विश्व में विविध प्रकार के संघर्ष विद्यमान हैं। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के समूह के बीच संघर्ष है। प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रयास रहता है कि वह व्यापारिक दृष्टि से अन्य राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। विभिन्न राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के समूह के बीच संघर्ष का अन्य कारण नृजातीयता अथवा धर्म हो सकता है। इजराइल एवं अरब देशों में संघर्ष इसी श्रेणी का उदाहरणं है। इसी भाँति, एक ही राष्ट्र के अंदर अनेक प्रकार के संघर्ष विद्यमाने हैं। इन संघर्षों का आधार वर्ग, जाति, जनजाति, लिंग, नृजातीयता, सांप्रदायिकता, भाषा, क्षेत्र इत्यादि हो सकता है। भारत में सांप्रदायिकता पर आधारित दंगे-फसाद होते हैं, जाति के आधार पर संघर्ष देखे जा सकते हैं, जनजातियाँ अपनी आकांक्षाएँ पूरी न होने पर आंदोलनरत हो जाती हैं। लिंग समता हेतु महिला आंदोलन न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी विकसित हुए हैं तथा इनका सामाजिक संरचना पर काफी प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रीय आधार पर भी संघर्ष अनेक नए राज्यों के निर्माण में प्रतिफलित होता है। भाषा के आधार पर होने वाले संघर्षों के कारण ही आज भी हिन्दी मातृभाषा होने के बावजूद सभी राज्यों में नहीं बोली जाती है। विकासशील देशों में नए तथा पुराने के बीच संघर्ष स्पष्ट देखते जा सकते हैं। प्राचीन प्रणाली नवीन शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, न ही लोगों की नवीन आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। संघर्ष बेकार की बहस, विभ्रान्ति, विसंगति तथा कई मौकों पर खून-खराबे को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी पद्धति संघर्षविहनी थी। पुरातन समय में भी जनसंख्या के बड़े भाग पर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे।
प्रश्न 16.
भूमि-संघर्ष से संबंधित वितरण में विभिन्न सामाजिक वर्गों को पहचानिए तथा शक्ति एवं संसाधनों की भूमिका पर ध्यान दीजिए। (क्रियाकलाप 10)
उत्तर-
भूमि-संघर्ष मुख्य रूप से भू-पतियों (भू-स्वामियों) तथा किसानों अथवा किसानों एवं साहूकारों के बीच होते रहे हैं। भारतीय कृषकों ने अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय कृषकों का साहूकारों एवं जमींदारों के दमन और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का लम्बा इतिहास रहा है। सम्पन्न कृषकों एवं भूमिहीन कृषकों में संघर्ष हो रहे हैं। टी०के० ओमन ने भूदान-ग्रामदान आंदोलन के अध्ययन में एक कृषक एवं साहूकार के बीच भूमि-संघर्ष का उल्लेख किया। हरबक्श नामक एके राजपूत ने 1956 ई० में नत्थू अहीर (पटेल) से १ 100 कर्ज के रूप में लिए तथा इसके लिए उसे अपने दो एकड़ जमीन को गिरवी रखना पड़ा। उसी वर्ष हरबक्श की मृत्यु हो गई उसके उत्तराधिकारी गणपत ने 1958 ई में जमीन को वापस लेने का दावा किया। इसके लिए उसने 200 देने की पेशकश की। नत्थू ने गणपत को जमीन वापस करने से मना कर दिया। गणपत इसके लिए कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं ले सका क्योंकि इस लेन-देन का कोई रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। इन परिस्थितियों के अधीन गणपत ने हिंसा का सहारा ले 1959 ई० (ग्रामदान के एक वर्ष पश्चात्) में जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया। गणपत, चूंकि स्वयं एक पुलिस कांस्टेबल था अतः इस मामले में उसने अफसरों पर काफी प्रभाव डाला। पटेल को पुलिस थाने में गणपत को जमीन वापस करने हेतु जबरन राजी कर लिया। इसके पश्चात् ग्रामवासियों की एक सभा बुलाई गई जिसमें पटेल को पैसा दिया गया और गणपत को अपनी जमीन वापस मिल गई।
प्रश्न 17.
सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया के आषसी संबंधों पर परिचर्चा कीजिए। (क्रियाकलाप 11)
उत्तर-
सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया में गहरा संबंध पाया जाता है। सामाजिक संरचना शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज संरचनात्मक है अर्थात् अपने विशिष्ट रूप में वह क्रमवार तथा नियमित है। सामाजिक संरचना की संकल्पना लोगों के आचरण, एक-दूसरे से संबंध में अंतर्निहित नियमितताओं को व्यक्त करती है। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। जिस प्रकार का संबंध सामाजिक संरचना एवं सामाजिक स्तरीकरण में है, ठीक उसी प्रकार का संबंध सामाजिक स्तरीकरण एवं प्रक्रियाओं में भी है। लिंग अथवा वर्ग जैसे सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधने जो प्रतिस्पर्धा सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, उन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकण के द्वारा आकार दिया जाता है। साथ ही, व्यक्ति पूर्वस्थित संरचना तथा स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।
प्रश्न 18.
क्रियाकलाप 11 तथा 12 में दिए गए उदाहरणों में जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है उसकी असमानताओं को देशाईए। (क्रियाकलाप 12)
उत्तर-
क्रियाकलाप 11 में संतोष एवं पुष्पा तथा क्रियाकलाप 12 में विक्रम एवं नितिन के उदाहरण दिए गए हैं जो सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया के आपसी संबंधों को दर्शाते हैं। संतोष एक भूमिहीन मजदूर का बेटा है जिसने अपनी पढ़ाई के लिए साहूकार र 8,000 का ऋण लिया। साहूकार के ऋण माँगने पर उसने गन्ने की फैक्ट्री के ठेकेदार से कुछ अग्रिम राशि आय के रूप में लेकर साहूकार के ऋण को चुकाया। ठेकेदार की ठेकेदारी के अंतर्गत काम करने के लिए उसने 14 वर्ष की पुष्पा से विवाह कर लिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि ठेकेदार अकेले लड़कों की बजाय विवाहित दंपति को काम देना पंसद करते हैं क्योंकि वे फैक्ट्री में ज्यादा महीनों तक रुककर काम करते हैं। 16 वर्ष की आयु में संतोष ने 10वीं कक्षा तथा पुष्पा ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त की। पुष्पा अपनी पढ़ाई तथा अपने डेढ़ वर्ष के बच्चे की देखभाल दोनों कार्यों के बीच संतुलन बनाकर करती है। इसके अतिरिक्त घर-परिवार तथा खेतों में भी काम होता है। उसके ससुराल वालों का कहना है कि वे कर सकते हैं जब उन्हें कोई छात्रवृत्ति मिले; अन्यथा यह दंपत्ति मुंबई के किसी निर्माण क्षेत्र में काम करने चले जाएँगे।
क्रियाकलाप 12 में तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन व्यापार के क्षेत्र . में बढ़ती हुई नौकरियों तथा काम के प्रति लोगों के बदलते हुए दृष्टिकोण का उदाहरण दिया गया है। कामकाजी वर्ग तुरंत अपने किए गए कार्यों के लिए इनाम चाहता है। उन्नति जल्दी-से-जल्दी मिलनी चाहिए और पैसा (अच्छी तनख्वाह, अतिरिक्त भत्ता तथा ऊँची वृद्धि) मुख्य उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। 27 वर्ष के विक्रम सामन्त ने अभी-अभी बी०पी०ओ में कार्यभार सँभला है; अपनी पिछली नौकरी को छोड़ देने का मुख्य कारण वह बेहतरीन तनख्वाह को मानता है। उसका कहना है कि उसके नए मालिक अच्छी तरह से जानते हैं कि वह हर उस एक रुपये के लिए काबिल है जो वे उसे देते हैं। इस नई अर्थव्यवस्था में कॉरपोरेट जगत की सीढ़ी पर एक-एक सीढ़ी न चढ़ते हुए ऊँची छलाँगें मारने की भी प्रवृत्ति बढ़ी है। नितिन ने आई०सी०आई०सी०आई० को छोड़कर एक तरक्की ले पहले अपने आप को स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जोड़ा तथा फिर ऑप्टिमिक्स में क्षेत्रीय मैनेजर का पद प्राप्त किया। नितिन का कहना है कि वह अगला पद जल्दी पाना चाहता है तथा इसके लिए बुढ़ापे तक इंजतार नहीं करना चाहता है।
उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में आधुनिक युग में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं में संबंध दर्शाया गया है। संतोष ने साहूकार का ऋण वापस करने हेतु गन्ने के ठेकेदार से पैसा लेकर पुष्पा से विवाह इसलिए किया ताकि ठेकेदार उसे ज्यादा दिनों तक नौकरी पर रख सके। पुष्पा पढ़ाई में होशियार होने के साथ-साथ अपने घर-परिवार तथा बाहर के कार्यों में तालमेल बनाए रखती है। संतोष का पुष्पा से विवाह करना उसकी मजबूरी थी तथा पुष्पा की मजबूरी कामकाजी होने के नाते बाहर तथा घर की भूमिका में संतुलन बनाए रखना था। दोनों में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा के अवसर सीमित विक्रम तथा नितिन जिस प्रतिस्पर्धा में लगे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य अच्छे वेतन के लिए बड़ी-बड़ी छलॉग लगाना है। वे जानते हैं कि इसके लिए उन्हें स्वयं इस योग्य बनना होगा ताकि मालिक पहली नौकरी की तुलना में अधिक वेतन दे सके। वे पूरी तरह से सोचते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मालिक अपने कर्मचारी को वेतन तथा वेतन वृद्धि उसकी योग्यता के आधार पर देता है। मालिक जानता है कि वह जो वेतन कर्मचारियों को दे रहा है, कर्मचारी उससे कहीं अधिक काम उसके लिए कर रहे हैं।
परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर
बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1.
निम्न में से कौन-सा जाति को आधार है?
(क) जन्म
(ख) कर्म
(ग) भाग्य
(घ) धन
उत्तर-
(क) जन्म
प्रश्न 2.
जाति की सदस्यता होती है
(क) अर्जित
(ख) जन्म से
(ग) दोनों
(घ) कोई नहीं
उत्तर-
(ख) जन्म से
प्रश्न 3.
निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है ?
(क) जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती
(ख) वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है,
(ग) भारतीय संविधान ने जातिवाद का समर्थन किया है।
(घ) जाति-व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है।
उत्तर-
(घ) जाति-व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है।
प्रश्न 4.
“एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है।” यह परिभाषा किसने दी है ?
(क) पी० एच० प्रभु ने
(ख) ब्लण्ट ने
(ग) एन० के० दत्ता ने
(घ) रिज़ले ने
उत्तर-
(ख) ब्लण्ट ने
प्रश्न 5.
जाति के लक्षणों में निम्नलिखित चार में कौन विशेष महत्त्वपूर्ण है ?
(क) श्रम-विभाजन
(ख) श्रेणीक्रम
(ग) अंतर्विवाह
(घ) खण्डनात्मकता
उत्तर-
(ग) अंतर्विवाह
प्रश्न 6.
निम्नलिखित में कौन-सी विशेषता जाति की नहीं है.?
(क) पेशा बदलने से जाति परिवर्तित हो जाती है।
(ख) जाति पेशे से संबंधित है।
(ग) जाति जन्म से निर्धारित होती है।
(घ) जाति अंतर्विवाही होती है।
उत्तर-
(क) पेशा बदलने से जाति परिवर्तित हो जाती है।
प्रश्न 7.
जाति को निर्धारण किससे होता है ?
(क) व्यवसाय से
(ख) जन्म से
(ग) क्षेत्र से
(घ) विवाह से
उत्तर-
(ख) जन्म से
प्रश्न 8.
‘कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया’ के लेखक हैं-
(क) अहमद इम्तियाज
(ख) जी0 एस0 घुरिये
(ग) राधा कमल मुखर्जी
(घ) सोरोकिन
उत्तर-
(क) अहमद इम्तियाज
प्रश्न 9.
‘द पीपुल ऑफ इंडिया’ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं ?
(क) सर हरबर्ट रिज़ले
(ख) चार्ल्स कूले
(ग) डॉ० जी० एस० घुरिये
(घ) मजूमदार एवं मदान
उत्तर-
(क) सर हरबर्ट रिज़ले
प्रश्न 10.
‘ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम’ पुस्तक किसने लिखी है?
(क) के० एम० कपाड़िया
(ख) योगेन्द्र सिंह
(ग) एस० सी० दूबे
(घ) नेसफील्ड
उत्तर-
(घ) नेसफील्ड
प्रश्न 11.
निम्नलिखित में कौन-सा वर्ग है ?
(क) पूँजीपति
(ख) हरिजन
(ग) श्रमिक संघ
(घ) युवा वर्ग
उत्तर-
(क) पूँजीपति
प्रश्न 12.
निम्नलिखित में कौन-सा वर्ग नहीं है?
(क) श्रमिक
(ख) लिपिक
(ग) बुद्धिजीवी
(घ) महिलाएँ
उत्तर-
(घ) महिलाएँ
प्रश्न 13.
‘कास्ट इन इंडिया’ पुस्तक का लेखक कौन है ?
(क) जे० एच० हट्टन
(ख) इरावर्ती कर्वे
(ग) एम0 एस0 दूबे
(घ) जी०एस० घुरिये
उत्तर-
(क) जे० एच० हट्टन
निश्चित उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
हरबर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया था?
उत्तर-
हरबर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक ‘प्रिसिंपल्स ऑफ़ सोशियोलॉजी’ में किया था।
प्रश्न 2.
इमाइल दुर्णीम ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया था?
उत्तर-
इमाइल दुर्णीम ने सर्वप्रथम ‘सामाजिक संरचना’ शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक ‘दि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड’ में किया था।
प्रश्न 3.
‘कास्ट इन इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
‘कास्ट इन इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम जे०एच० हट्टन है।
प्रश्न 4.
‘कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
कास्ट एंड रेस इन इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम जी०एस० घुरिये है।
प्रश्न 5.
‘कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन’ पुस्तक के लेखक का नाम जी०एस० घुरिये है।
प्रश्न 6.
‘सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
‘सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम एम०एन० श्रीनिवास है।
प्रश्न 7.
‘कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अंदर ऐसेज’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
इस पुस्तक के लेखक का नाम एम०एन० श्रीनिवास है।
प्रश्न 8.
‘रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम डी०एन० मजूमदार है।
प्रश्न 9.
‘कास्ट, क्लास एंड पावर’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
‘कास्ट, क्लास एंड पावर’ पुस्तक के लेखक का नाम आंद्रे बेतेई है।
प्रश्न 10.
‘कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर-
कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया’ पुस्तक के लेखक का नाम पी० कोलंडा है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
सामाजिक संरचना की उपयुक्त परिभाषा दीजिए।
उत्तर-
टॉलकॉट पारसंस के अनुसार, “सामाजिक संरचना से तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है। पारसंस की इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक संरचना एक विशिष्ट क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसकी प्रमुख इकाइयाँ संस्थाएँ, अभिकरण, प्रतिमान और समूह हैं जो एक-दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित स्थिति और भूमिका होती है। इस स्थिति और भूमिका को निर्धारण सामाजिक संस्थाएँ ही करती हैं। इन्होंने इसे एक अमूर्त धारणा के रूप में समझने का प्रयास किया है।
प्रश्न 2.
सामाजिक संरचना की.दो प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
उत्तर-
सामाजिक संरचना की दो प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—
- अमूर्त अवधारणा–सामाजिक संरचना कोई वस्तु या व्यक्तियों का संगठन नहीं है। यह तो मात्र प्रतिमानों, संस्थाओं, नियमों, कार्यप्रणालियों व पारस्परिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है। अतः यह एक अमूर्त धारणा है।
- समाज के बाह्य ढाँचे का बोध-सामाजिक संरचना से समाज के बाह्य स्वरूप मात्र का बोध होता है। यह इकाइयों की क्रमबद्धता से संबंधित है, न कि इनके कार्यों से।
प्रश्न 3.
सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं?
उत्तर-
सामाजिक प्रक्रिया से अभिप्राय सामाजिक अंत:क्रिया के विभिन्न स्वरूपों से है। यह परस्पर संबंधित घटनाओं का एक क्रम है जिसे हम विशिष्ट परिणाम और परिवर्तन को जन्म देने वाला मानते हैं। फेयरचाइल्ड ने समाजशास्त्र के शब्दकोश में सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा इन शब्दों में दी है-“कोई भी सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया, जिसमें अवलोकनकर्ता एक सतत (निरत) गुण या दिशा देखता हो, जिसे एक वर्गीय नाम दिया जा सके, सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया का एक वर्ग जिसमें सामान्य रूप से सामान्य आदर्श देखा जा सके व नामांकित किया जा सके। उदाहरणार्थ-अनुकरण, पर-संस्कृतिग्रहण, संघर्ष, सामाजिक नियंत्रण, संस्तरण।”
प्रश्न 4.
सामाजिक प्रक्रिया की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए।
उत्तर-
गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, “सामाजिक प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय अंत:क्रिया के उन तरीकों से है जिनका हम, जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था करते हैं या जब जीवन के पूर्व-प्रचलित तरीकों में परिवर्तन के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अवलोकन कर सकते हैं।”
प्रश्न 5.
सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकार कौन-से हैं?
उत्तर-
सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं-
- सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ–सहयोगी प्रक्रियाओं को सहगामी प्रक्रियाएँ, संगठनात्मक प्रक्रियाएँ या एकीकरण लाने वाली प्रक्रियाएँ भी कहा जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य सहयोग में वृद्धि करना है। सहयोग, व्यवस्थापन तथा सात्मीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
- असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ–असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं को असहगामी, विघटनकारी या पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएँ भी कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष इसके उदहारण हैं।
प्रश्न 6.
सहयोग एवं प्रतियोगिता की एक-एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए।
उत्तर-
फिचर के अनुसार, “सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या समूह एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।” ग्रीन के अनुसार, “प्रतियोगिता में दो या अधिक व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय करते हैं जिसको कोई भी दूसरों के साथ बाँटने के लिए न तो तैयार होता है और न ही इसकी अपेक्षा की जाती है।”
प्रश्न 7.
संघर्ष किसे कहते हैं?
उत्तर-
संघर्ष एक चेतन एवं असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के हितों को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तथा बलपूर्वक एक-दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उनसे कोई काम लेना चाहते हैं। कोजर के अनुसार, “स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है जिनमें विरोधी दलों का उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धी को प्रभावहीन करना, हानि पहुँचाना अथवा समाप्त करना भी है।”
प्रश्न 8.
वर्ग किसे कहते हैं?
या
वर्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
जब एक ही सामाजिक स्थिति के व्यक्ति समान संस्कृति के बीच रहते हैं तो वे एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी सामाजिक स्थिति लगभग समान हो और जो एक-सी ही सामाजिक दशाओं में रहते हों। एक वर्ग के सदस्य एक जैसी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। एक-सी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों को एक वर्ग विशेष का नाम दे दिया जाता है; जैसे-पूँजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार, “सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक योग है जिनका किसी समाज में निश्चित रूप से एक समान स्तर होता है।”
प्रश्न 9.
जाति की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए।
या
जाति के अर्थ को स्पष्ट करने वाली कोई सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा बताइए।
उत्तर-
जाति’ शब्द जितना सरल लगता है इसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन कार्य है। अधिकांश विद्वानों ने जाति की परिभाषा इसकी प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर दी है। उदाहरणार्थ-बलंट के अनुसार, “एक जाति एक अंतर्विवाह वाला समूह है या अंतर्विवाह करने वाले समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता वंशानुगत होती है, जो अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाता है, एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करता है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है और आमतौर से एक सजातीय समुदाय को बनाने वाला समझा जाता है। जाति की यह परिभाषा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जा सकती है क्योंकि इसमें जाति की सभी प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखा गया है।
प्रश्न 10.
जाति तथा वर्ग में पाए जाने वाले दो प्रमुख अंतर बताइए।
उत्तर-
जाति तथा वर्ग में पाए जाने वाले दो प्रमुख अंतर निम्न प्रकार हैं—
- प्रकृति में अंतर-वर्ग में मुक्त संस्तरण होता है अर्थात् व्यक्ति वर्ग परिवर्तन कर सकता है। जाति में बंद संस्तरण होता है अर्थात् जाति का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- सदस्यता में अंतर-वर्ग की सदस्यता व्यक्तिगत योग्यता, जीवन के स्तर एवं हैसियत आदि पर आधारित होती है। जातिं की सदस्यता जन्म से ही निश्चित हो जाती है।
लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं?
या
सामाजिक संरचना किसे कहते हैं?
उत्तर-
सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा मानी जाती है। संमाज विभिन्न संस्थाओं, समूहों, वर्गों, परंपराओं और रीति-रिवाजों के योग से बनता है। ये सभी बातें मिलकर समाज को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करती हैं। इसी क्रमबद्ध स्वरूप को ‘सामाजिक संरचना का नाम दिया जाता है। अन्य शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो समाज विशेष में और एक समय विशेष पर सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः संरचना से तात्पर्य व्यवस्थित ढाँच से है। सामाजिक संरचना में संगठन का होना जरूरी है। बिना संगठन के सामाजिक संरचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती। सामाजिक संरचना में किसी वस्तु या समाज के विभिन्न अंगों के बीच पायी जाने वाली सुव्यवस्था का बोध होता है। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित जाल, जिससे समाज का निर्माण होता है, सामाजिक संरचना का मूल आधार है। रैडक्लिफ-ब्राउन के अनुसार, “सामाजिक संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की जा सकती है।”
प्रश्न 2.
जाति किसे कहते हैं?
या
जाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म लेने वाले समूह से निर्धारित होती है। जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है। जाति कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों को मानने वाला वह समूह है। जिसके सदस्यों में रक्त शुद्धि होने का विश्वास पाया जाता है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्रापत कर लेता है और आजन्म उसकी सदस्यता को त्याग नहीं सकता है। इस प्रकार का समूह सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है। इस समूह के सदस्य अन्य किसी समूह के सदस्य नहीं होते हैं और न कोई बाहर के समूह के सदस्य इस समूह के सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार जाति एक बंद वर्ग है। ‘जाति’ शब्द अंग्रेजी के ‘कास्ट’ (Caste) शब्द का हिंदी अनुवाद है जो पुर्तगाली भाषा के ‘कास्टा (casta) शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है नस्ल, प्रजाति या भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1565 ई० में गार्सिया दी ओरटा ने किया था। समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। रिजले के अनुसार, जाति ऐसे परिवारों या परिवार-समूहों का संकलन है, जिनका उनके विशिष्ट पेशों के अनुसार एक सामान्य नाम हो, जो एक ही पौराणिक पितामह-मनुष्य या देवता से अपनी उत्पत्ति मानते हों तथा जो एक ही व्यवसाय करते हों।”
प्रश्न 3.
लैगिक असमता से आप क्या समझते हैं?
उत्तर-
जन्म के समय शिशु के लिंग को लेकर यदि समाज किसी प्रकार का भेदभाव करता है तो उसे हम लैंगिक असमता कहते हैं। यह लैंगिक असमता एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य बन चुकी है क्योकि सभी समाजों में इसका कोई-न-कोई रूप देखा जा सकता है। लड़का या लड़की होना तो एक जैवकीय तथ्य है, परंतु इनमें से किसी एक को ऊँचा या नीचा स्थान देना एक सामाजिक तथ्य है।
अधिकांश समाजों के पितृसत्तात्मक होने के कारण जन्म के साथ ही लिंग के आधार पर भेदभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। अधिकांशतया लड़के को लड़की से ऊँचा स्थान दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि लड़के के जन्म पर अधिकांश लोग खुशियों मनाते हैं तथा दावतें देते हैं, जबकि लड़की के जन्म पर ऐसा बहुत कम किया जाता है। लैंगिक असमता के कारण ही पितृसत्तात्मक समाजों में लड़के को ऊँचा माना जाता है, तो मातृसत्तात्मक परिवारों में लड़की को लड़के से ऊँचा स्थान दिया जाता है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1.
सामाजिक संरचना किसे कहते हैं? इसके प्रमुख तत्त्व एवं विशेषताएँ बताइए।
या
सामाजिक संरचना की परिभाषा दीजिए। इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
या
सामाजिक संरचना की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की वह व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो कि समाज विशेष में और एक समय में सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबंद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अतः संरचना से तात्पर्य व्यवस्थित ढाँचे से है। सामाजिक संरचना में संगठन का होना जरूरी है। बिना संगठन के सामाजिक संरचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती।
सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषाएँ
सामाजिक संरचना से किसी वस्तु या समाज के विभिन्न अंगों के बीच पायी जाने वाली सुव्यवस्था की बोध होता है। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित जाल, जिससे समाज का निर्माण होता है, सामाजिक संरचना का मूल आधार है। इसे विद्वानों ने निम्न प्रकारे से परिभाषित किया है-
रैडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) के अनुसार-“संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की जा सकती है।” रैडक्लिफ-ब्राउन के अनुसार, “सामाजिक संरचना के प्रमुख अंग मनुष्य ही हैं। व्यक्तियों के संस्थागत रूप से परिभाषित तथा नियमित संबंधों की क्रमबद्ध व्यवस्था को ही सामाजिक संरचना कहलाती है।
टॉलकट पारसन्स (Talcott Parsons) के अनुसार-“सामाजिक संरचना से तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है।”
पारसंस के अनुसार, सामाजिक संरचना एक विशिष्ट क्रमबद्ध व्यवस्था है जिसकी प्रमुख इकाइयाँ संस्थाएँ, अधिकरण, प्रतिमान और समूह हैं जो एक-दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित स्थिति और भूमिका होती है। इस स्थिति और भूमिका का-निर्धारण सामाजिक संस्थाएँ ही करती हैं। इन्होंने इसे एक अमूर्त धारणा के रूप में समझने का प्रयास किया है।
कार्ल मैनहिम (Karl Mannheim) के अनुसार-“सामाजिक संरचना अंत:क्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे विभिन्न प्रकार की अवलोकन और विचार-पद्धतियों का जन्म हुआ है।” मैनहिम के अनुसार, संरचना अंत:क्रियात्मक शक्तियों का जाल है। सामाजिक शक्तियों से तात्पर्य उन नियमों या नियंत्रण के साधनों से है जो व्यक्ति और समूह के सामाजिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करते हैं और स्थायित्व प्रदान करते हैं। इन सामाजिक शक्तियों की पारस्परिक अंत:क्रिया से ही सामाजिक ढाँचे का निर्माण होता है जिसे मैनहिम सामाजिक संरचना कहता है।
जिंसबर्ग (Ginsberg) के अनुसार-“सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, अर्थात् समितियों, समूह तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी सम्पूर्ण जटिलता, जिससे कि समाज का निर्माण होता है, से संबंधित है।” जिंसबर्ग ने मैनहिम के विपरीत सामाजिक संरचना की परिभाषा में इसकी निर्णायक इकाईयों को आधार माना है। सामाजिक संरचना समितियों, समूहों तथा संस्थाओं के सुव्यवस्थित योग को कहते हैं। यह एक जटिल संकुल है।
एस०एफ० नैडल (S.F Nadel) के अनुसार-“सामाजिक संरचना शब्द की चर्चा हरबर्ट स्पेंसर व दुर्णीम की रचनाओं में मिलती है। साथ ही आधुनिक साहित्य में भी इसकी चर्चा को नहीं छोड़ा गया है। किंतु इसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया गया है जिससे समाज को निर्मित करने वाली किसी एक अथवा समस्त विशेषताओं का बोध होता है। इस प्रकार यह शब्द किसी व्यवस्था, संगठन संकुल, प्रतिमान या प्रारूप, यहाँ तक कि समग्र समाज का पर्यायवाची हो जाता है। नैडल ने सामाजिक संरचना को अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता कहा है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से तो स्थिर होती है परंतु इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। यद्यपि यह एक विरोधाभास प्रतीत होता है फिर भी इस परिभाषा को काफी मान्यता प्राप्त है। वास्तव में नैडल के अनुसार सामाजिक संरचना कुछ विशिष्ट प्रकार के सामाजिक प्रतिमानों अथवा सामाजिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है जिसमें बहुत ही कम परिवर्तन होने की संभावना होती है।
मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार-“समूह निर्माण के विभिन्न स्वरूप संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक श्रेणियों की विभिन्न मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रदर्शित होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक समूहों के निर्माण के विभिन्न तरीकों के सम्मिलित रूप को सामाजिक संगठन कहा गया है और यही संगठन सामाजिक संरचना का आधार माना जाता है। इन्होंने इसे एक अमूर्त अवधारणा माना है। जिस प्रकार हम समाज को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार हम इसकी संरचना को भी नहीं देख सकते हैं। संपूर्ण संरचना एक अखंड व्यवस्था न होकर विभिन्न अंगों से निर्मित होने वाली व्यवस्था है।
हैरी एम० जॉनसन (Harry M. Johnson) के अनुसार-“किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंत:संबंधों को कहते हैं।’
जॉनसन के अनुसार भी सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है अपितु इसका निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है। इसके निर्णायक अंग परस्पर क्रमबद्ध रूप से संबद्ध होते हैं और इसी कारण संरचना में अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता है। सामाजिक संरचना के अंग भी अधिक परिवर्तनशील नहीं होते हैं। अत: सामाजिक संरचना यद्यपि परिवर्तनशील प्रकृति की हो सकती है परंतु फिर भी यह एक अपेक्षाकृत स्थिर अवधारणा है जो विभिन्न अंगों से मिलकर निर्मित होती है।
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक संरचना से अभिप्राय किसी इकाई के अंगों की क्रमबद्धता है। समाज में व्यक्ति आपसी संबंधों में बँधकर उपसमूहों का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न उपसमूह आपस में बाँधकर समूहों का निर्माण करते हैं।
सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्त्व
सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं-
- सामाजिक आदर्श–बिना आदर्शों के हम सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्हीं से व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है।
- सामाजिक स्थिति इसे सामाजिक संरचना की लघुतम इकाई कहा गया है। यह समूह द्वारा व्यक्ति को दिया गया पद है।
- सामाजिक भूमिका—यह स्थिति का गत्यात्मक पहलू है जिससे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आचरण का पता चलता है।
सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएँ
विभिन्न परिभाषाओं से सामाजिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं-
- अर्भूत अवधारणा–सामाजिक संरचना कोई वस्तु या व्यक्तियों का संगठन नहीं है। यह तो केवल मात्र प्रतिमानों, संस्थाओं, नियमों, कार्यप्रणालियों व पारस्परिक संबंधों की एक क्रमबद्धता है। अतः यह एक अर्मूत धारणा है।
- समाज के बाह्य ढाँचे का बोध-सामाजिक संरचना से समाज के बाह्य स्वरूप मात्र का बोध होता है। यह इकाइयों की क्रमबद्धती संबंधित है, न कि इसके कार्यों से। जिस प्रकार शरीर की संरचना से तात्पर्य उसके अंगों की क्रमबद्धता से है उनके क्रियाकलापों से नहीं, उसकी प्रकार सामाजिक संरचना का संबंध इसकी इकाइयों की क्रमबद्धता से है।
- स्थिर धारणा–सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थिर धारणा है क्योंकि इसकी निर्माणक इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और उनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। जॉनसन जैसे विद्वान् इसे परिवर्तनशील प्रकृति का मानते हुए भी इसे एक स्थिर अवधारणा कहते हैं।
- प्रत्येक समाज की संरचना में भिन्नता–सभी समाजों की सामाजिक संरचना एक जैसी नहीं होती है अपितु प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। इसीलिए समाजों की संस्थाओं व रीति-रिवाजों में भी अंतर होता है।
- सामाजिक व्यवस्था का आधार स्तंभ-सामाजिक संरचना को सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार माना जाता है। जब संरचना की इकाइयाँ अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभाती हैं तो सामाजिक व्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है। जैसे ही इकाइयाँ अपनी स्थिति के अनुकूल भूमिका निभाता बंद कर देती हैं तो सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। सामाजिक संरचना इस प्रकार सामाजिक संगठन को सुदृढ़ भी बनाती है।
- अनेक उपसंरचनाएँ-सामाजिक संरचना कोई अखंड व्यवस्था न होकर अनेक उपसंरचनाओं द्वारा निर्मित होती है। विभिन्न उपसंरचनाएँ मिलकर सम्पूर्ण सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। इसकी उपसंरचनाओं अथवा अंगों की स्वयं में भी एक विशिष्ट संरचना हो सकती है।
- विभिन्न अंगों को योग-संरचना के विभिन्न अंग होते हैं जिनमें सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक स्थितियों व भूमिकाओं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग निश्चित ढंग से व्यवस्थित रहते हैं और एक-दूसरे से संबंधित होते हैं।
निष्कर्ष–सामाजिक संरचना की विभिन्न परिभाषाओं तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह समाज के विभिन्न अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता है जो किसी समाज में समय विशेष में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, प्रस्थितियों, भूमिकाओं उपकरणों तथा सामाजिक प्रतिमानों के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप विकसित होती है।
प्रश्न 2.
सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? सामाजिक प्रक्रियाएँ कौन-सी हैं
या
सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए।
उत्तर-
जब समूह, समुदाय या समाज के सदस्य परस्पर व्यवहार करते हैं तो उनमें निश्चित व अर्थपूर्ण अंत:क्रियाएँ विकसित होती हैं। समूह के सदस्यों में पायी जाने वाली अंत:क्रियाएँ सहयोग के रूपमें हो सकती हैं अथवा संघर्ष के रूप में भी हो सकती हैं। उनमें प्रतियोगिता हो सकती है और समायोजन तथा व्यवस्थापन भी हो सकता है। सामाजिक अंत:क्रिया के इन विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक प्रक्रियाएँ सामाजिक संबंधों के अध्ययन की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं तथा विभिन्न प्रकार के संबंधों को बताती हैं। सामाजिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक संबंधों का होना जरूरी है। वास्तव में, सामाजिक संबंध परिवर्तनशील होते हैं परन्तु फिर भी इनमें निरंतरता पायी जाती है। इसीलिए सामाजिक संबंध, परिवर्तनशीलता तथा निरंतरता; सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण करने वाले तीन तत्त्व माने जाते हैं।
सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ एवं परिभाषाएँ
प्रमुख विद्वानों ने सामाजिक प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है-
- फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्र के शब्दकोश में सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा इन शब्दों में दी है-“कोई भी सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया जिसमें अवलोकनकर्ता एक सतत (निरत) गुण या दिशा देखता हो, जिसे एकवर्गीय नाम दिया जा सके, सामाजिक परिवर्तन या अंत:क्रिया का एक वर्ग जिसमें सामान्य रूप से सामान्य आदर्श देखा जा सके व नामांकित किया जा सके। उदाहरण के लिए अनुकरण, परसंस्कृतिग्रहण, संघर्ष सामाजिक नियंत्रण संस्तरण।”
- मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार-“एक प्रक्रिया से तात्पर्य परिस्थिति में पहले से विद्यमान शक्तियों के कार्यरत होने से एक निश्चित तरीके से होने वाले निरंतर परिवर्तन से है।”
- लंडबर्ग एवं सहयोगियों (Lundberg and Others) के अनुसार--“प्रक्रिया से तात्पर्य एक अपेक्षाकृत विशिष्ट और पूर्वानुमानित परिणाम की ओर से जाने वाली संबंधित घटनाओं के क्रम से है।”
- गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार–“सामाजिक प्रक्रिया से हमारी अभिप्राय अंत:क्रिया के उन तरीकों से है जिनका हम, जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं या जब जीवन के पूर्व प्रचलित तरीकों में परिवर्तन के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अवलोकन कर सकते हैं।”
- वान वीज (Von Wiese) के शब्दों में-“सामाजिक प्रक्रिया किसी भी सामाजिक संबंध का परिवर्तनशील पहलू है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हम सामाजिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम उस तरीके की बात करते हैं जिससे समूह के सदस्यों के संबंध में निश्चित तथा विशिष्ट लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। प्रक्रिया के अध्ययन में हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की श्रृंखला देखते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएँ उन्नति लाने वाली या पतन को प्रोत्साहन देने वाली, प्रगति या अवनति लाने वाली अथवा एकीकरण या विघटन की ओर ले जाने वाली होती हैं।
सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएँ
सामाजिक प्रक्रिया के अर्थ तथा विभिन्न विद्वानों के विचारों से इसकी जो प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं वे निम्नलिखित हैं-
- घटनाओं से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं का संबंध सामाजिक घटनाओं या सामाजिक संबंधों से है। बिना सामाजिक घटनाओं या सामाजिक संबंधों के हम सामाजिक प्रक्रिया की , कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
- निश्चित क्रम-सामाजिक प्रक्रिया केवल सामाजिक घटनाओं से ही संबंधित नहीं होती अपितु सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं का एक निश्चित क्रम का होना भी जरूरी है। किसी एक घटना को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।
- पुनरावृत्ति-सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक संबंधों के क्रम में पुनरावृत्ति होती रहती है। अर्थात् इनमें क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। पुनरावृत्ति के बिना किसी घटना को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।
- पारस्परिक संबद्धता–सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं अथवा संबंधों का परस्पर संबद्ध होना भी जरूरी है। उनकी प्रकृति तथा क्षेत्र अलग-अलग होते हैं परन्तु उनका परस्पर संबद्ध होना सामाजिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है।
- निरंतरता-सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं तथा संबंधों में निरंतरता होना भी आवश्यक है। अगर इसमें पुनरावृत्ति होती है परंतु निरंतरता नहीं पायी जाती तो इसे सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जाएगा।
- विशिष्ट परिणाम-सामाजिक प्रक्रियाएँ मानवीय अंत:क्रियाओं का अवश्यम्भावी परिण्षम होती हैं। इनके कुछ-न-कुछ परिणाम अवश्य होते हैं चाहे वे संगठन के लिए उपयोगी हों अथवा नहीं।
- अनेक रूप-सामाजिक प्रक्रियाओं के अनेक रूप होते हैं। जिन प्रक्रियाओं द्वारा समाज में सहयोग व संगठन बना रहता है उन्हें सहयोगी प्रक्रियाएँ कहते हैं और जिनके द्वारा पृथक्करण की प्रवृत्ति विकसित होती है, उन्हें असहयोगी प्रक्रियाएँ कहा जाता है।
- अन्योन्याश्रितता–सामाजिक प्रक्रियाओं की एक अन्य विशेषता अन्योन्याश्रितता है। इसका अभिप्राय यह है कि अभी प्रक्रियाएँ परस्पर अंत:संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं।
- संरचना और कार्यों से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाएँ सामाजिक संरचना और कार्यों से सबंधित होती हैं क्योंकि इनका प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक संरचना तथा इसका निर्माण करने वाली इकाइयों के कार्यों पर पड़ता है।
सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार
सामाजिक प्रक्रियाओं का कोई रूप नहीं है अपितु ये अनेक प्रकार की होती हैं। इनके परिणामों के आधार पर समाजशास्त्रियों ने इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है–
(अ) सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ तथा
(ब) असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ।
सहयोगी प्रक्रियाओं को सहभागी प्रक्रियाएँ, संगठनात्मक प्रक्रियाएँ या एकीकरण लाने वाली प्रक्रियाएँ भी कहा जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य सहयोग में वृद्धि करना है। सहयोग, व्यवस्थापन तथा सात्मीकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं को असहगामी, विघटनकारी या पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएँ भी कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष इसके उदाहरण हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रकारों को निम्नांकित चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-
सहयोगी व्यवस्थापन सात्मीकरण प्रतिस्पर्धा प्रतिकूलन संघर्ष सहयोग (Co-operation) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह अपने संयुक्त प्रयत्नों को अधिक या कम संगठित रूप से, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित करते हैं। यह सामान्य उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना है। समाज का विशाल भवन सहयोग की मजबूत नींव पर खड़ा है। सहयोगी या सहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग सर्वोपरि व अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। सहयोग के बिना न तो पीढ़ियों का समाजीकरण ही ठीक प्रकार से हो सकता है और न ही व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से किसी-न-किसी रूप में सहयोग की आवश्यकता पड़ती हैं। सहयोग द्वारा ही सामाजिक संगठन सुदृढ़ होता है।
फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्रीय शब्दकोश में सहयोग की परिभाषा इन शब्दों में दी है, “सामाजिक अंत:क्रिया का कोई भी वह स्वरूप; जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी क्रियाओं को संयुक्त कर लेते हैं या पारस्परिक सहायता से, कम या अधिक रूप में संगठित, तरीके से किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य या प्राप्ति के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं; सहयोग कहलाता है।”
व्यवस्थापन (Accommodation) भी सामाजिक अंत:क्रिया का एक स्वरूप तथा सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रमुख प्रकार है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतियोगी व्यक्ति या संघर्षरत समूह हितों में विरोध व संघर्ष से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने संबंधों को एक-दूसरे से समायोजित कर लेते हैं। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक देश तथा संस्कृति में पायी जाती है। यह सात्मीकरण (Assimilation) की ओर पहला कदम है क्योंकि इसमें एक संस्कृति दूसरी को आत्मसात् करने की अपेक्षा उससे अनुकूलन कर लेती है। अनुकूलन और समायोजन की इस प्रक्रिया को ही व्यवस्थापन कहा जाता है।
व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना उत्पन्न कर लेता है। इसके द्वारा और समुह सहयोगी एकता की स्थापना के लिए विरोधपूर्ण प्रक्रियाओं से सामंजस्य कर लेते हैं। यह एक दशा भी है क्योंकि व्यवस्थापन संबंधों की वह स्वीकृति या मान्यता है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति की स्थिति अथवा सम्पूर्ण सामाजिक संगठन में समूह की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार, “व्यवस्थापन से अभिप्राय विशेष रूप से उस प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना उत्पन्न कर लेता है।’
सात्मीकरण या आत्मसात् (Assimilation) एक सहयोगी प्रक्रिया है तथा वह सामाजिक संपर्को का अंतिम प्रतिफल है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्तियों या समूहों में पारस्परिक मतभेद दूर होते हैं तथा उनके दृष्टिकोणों में समानता विकसित होती है। वास्तव में, इस प्रक्रिया द्वारा दो समूह या संस्कृतियाँ एक-दूसरे में इस प्रकार घुल-मिल जाती हैं कि उनमें किसी प्रकार का अंतर ही नहीं रहता। इसीलिए सात्मीकरण को दृष्टिकोण और मूल्यों का संपूर्ण मिश्रण तथा सामाजिक संपर्को का अंतिम प्रतिफल कहा गया है। यह प्रक्रिया व्यवस्थापन से अगला चरण है क्योंकि इससे अस्थायी समझौता न होकर दो समूह या संस्कृतियाँ पूरी तरह से एक-दूसरे में घुल-मिल जाती हैं।
जब दो व्यक्ति, समूह या संस्कृतियाँ एक-दूसरे के व्यवहार और आदर्शों को स्वीकार कर लेते हैं तथा एक-दूसरे से इस प्रकार घुल-मिल जाते हैं कि उनमें कोई अंतर ही न रहे तो उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। यह दो भिन्न समूहों या संस्कृतियों के दृष्टिकोणों एवं मूल्यों का संपूर्ण सम्मिश्रण है।
ऑगबर्न एवं निमकॉफ (Ogburn and Nimkoff) के अनुसार, “सात्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा असमान व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं अर्थात् वे अपने स्वार्थों और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। ऑगर्बन एवं निमकॉफ की इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सात्मीकरण भावनाओं, उद्देश्यों, मूल्यों व दृष्टिकोणों में समानता लाने की प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप दो भिन्न समूह एक समान हो जाते हैं। इनके अनुसार यह संस्कृतियों या उनको धारण करने वाले व्यक्तियों का एक समान इकाई के रूप में घुल-मिल जाना हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्कृतियाँ एक हो जाती हैं।
प्रतिस्पर्धा (Competition) असहयोगी प्रक्रिया है। यह निर्मित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की होड़, जो इतनी अपर्याप्त मात्रा में है जिससे माँग की पूर्ति नहीं हो सकती है, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। यह अवैयक्तिक, अचेतन और निरंतर होने वाला संघर्ष है।
प्रतिकूलन या विरोध (Contravention) भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच की स्थिति है। इसके द्वारा व्यक्ति विरोधी वातावरण में दुविधा की स्थिति में पड़ जाता है। और इससे वह मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है।
संघर्ष (Conflict) एक अंसहयोगी प्रक्रिया है जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते है, भले हो इसके लिए उन्हें दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े। यह एक प्रकार से दूसरों का, दूसरों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना, रोकना तथा उसे (उन्हें) बलपूर्वक रोकने का प्रयास है। सहयोग की तरह संघर्ष भी सामाजिक जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सहयोग के बिना संघर्ष तथा संघर्ष के बिना सहयोग की कल्पना केवले सैद्धांतिक रूप में ही की जा सकती है। यह एक ऐसी असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंद्वी समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा तक का सहारा लेते हैं। वास्तव में यह दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक रोकने का प्रयास है। फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्रीय शब्दकोश में संघर्ष की परिभाषा इन शब्दों में दी है, “संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े।”
निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ सामाजिक अंत:क्रिया का वह स्वरूप है जो विशिष्ट होता है तथा जिसमें निरंतरता पायी जाती है। प्रक्रियाएँ सहयोगी व असहयोगी दोनों प्रकार की होती हैं।
प्रश्न 3.
सहयोग किसे कहते हैं इसके प्रमुख प्रकार बताइए।
या
सहयोग को परिभाषित कीजिए तथा समाज में इसका महत्त्व समझाइए।
उत्तर-
सहयोग को समाज की एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। यद्यपि समाज के लिए सहयोग के साथ-साथ संघर्ष भी महत्त्वपूर्ण होता है, तथापि समाज के अस्तित्व के लिए सहयोग प्राथमिक है। सहयोग द्वारा ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा यह परिवार से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय जीवन तक देखा जा सकता है। आज के जटिल समाजों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता व संघर्ष के कारण सहयोग का महत्त्व और भी अधिक हो गया। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के बिना हम आधुनिक समाजों में सामाजिक जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं।
सहयोग का अर्थ एवं परिभाषाएँ
सहयोग के सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। समाज का विशाल सहयोग की मजबूत नींव पर ही खड़ा होता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सहयोग के बिना संभव नहीं है। सहयोग को प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है-
फेयरचाइल्ड (Fairchild) ने समाजशास्त्रीय शब्दकोश में सहयोग की परिभाषा इन शब्दों में दी है-“सामाजिक अंतःक्रिया का कोई भी वह स्वरूप; जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी क्रियाओं को संयुक्त कर लेते हैं या पारस्परिक सहायता से, कम या अधिक रूप में संगठित तरीके से किसी सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं; सहयोग कहलाता है।”
सदरलैंड एवं वुडवर्ड (Sutherland and woodward) के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए परस्पर मिलकर कार्य करना सहयोग है।
ग्रीन (Green) के अनुसार-“दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्य को करने या किसी उद्देश्य, जो कि समान रूप से इच्छित होता है, तक पहुँचने के निरंतर और सामान्य प्रयत्न को सहयोग कहते हैं। सहयोग हमेशा एक सामूहिक कार्य होता है।”
फियर (Fichter) के अनुसार-“सहयोग एक सामाजिक प्रकिया का वह स्वरूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं।”
लुडबर्ग एवं सहयोगियों (Lundberg and Others) के अनुसार–-‘सहयोग से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह को लक्ष्य-प्राप्ति के लिए इस प्रकार साथ-साथ कार्य करना कि एक व्यक्ति या समूहों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति दूसरे व्यक्ति या समूह की भी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो।”
अकोलकर (Akolkar) के अनुसार-‘सहयोगी व्यवहार का सारतत्त्व यह है कि संबंधित व्यक्तियों या समूह को एक सामान्य लक्ष्य होता है और अपने व्यवहार का अनुकूलन एक-दूसरे के साथ इस भाँति करते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि सहयोग सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को मिलजुलकर कार्य करना है। यह सामाजिक अंतःक्रिया का एक प्रमुख स्वरूप है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ-साथ कार्य करते हैं।
सहयोग की प्रमुख विशेषताएँ
सहयोग के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों से इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं-
- सहयोग एक प्रमुख सहयोगी प्रक्रिया है।।
- यह एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि संघर्ष से विपरीत है।
- सहयोग द्वारा व्यक्ति या समूह सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
- सहयोग में सदस्यों के कार्यों का संयुक्तीकरण होता है।
- सहयोग में सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं।
- सहयोग में सदस्यों में हम की भावना पायी जाती है।
- सहयोग में मिलकर काम करने की भावना पायी जाती है।
- सहयोग में सदस्य संगठित रूप से सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं।
- सहयोग एक सामूहिक प्रयास है।
- सहयोग करने वाले एक-दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं।
किंबल यंग (Kimball Young) ने सहयोग के तीन प्रमुख पहलू बताए हैं-
- सदस्यों में सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा,
- प्राप्त लक्ष्यों या उद्देश्यों का समान अनुपात में विभाजन, तथा
- सदस्यों में महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं एवं कामनाओं में समानता, सहानुभूति तथा मित्रता का पाया जाना।
सहयोग के विभिन्न स्वरूप
सहयोग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सार्वभौमिक है क्योंकि कोई भी समाज सहयोग के बिना अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में सहयोग पाया जाता है। इसे प्रमुख विद्वानों द्वारा निम्नांकित रूपों में वर्गीकृत किया गया है–
(अ) मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) द्वारा वर्गीकरण
मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को निम्नलिखित दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजन किया है-
- प्रत्यक्ष सहयोग-प्रत्यक्ष सहयोग आमने-सामने के संबंधों में पाया जाता है। इसमें लोग मिलजुलकर एक-दूसरे की सहायता करते हैं। जिन कार्यों को व्यक्ति अकेला भी कर सकता है। उनको प्रत्यक्ष सहयोग द्वारा अधिक सरलता से पूरा किया जा सकता है। टीम के खिलाड़ियों का , एक-दूसरे से सहयोग, किसानों का साथ-साथ खेत जोतना, एक साथ अनेक लोगों का श्रम करना आदि प्रत्यक्ष सहयोग के कुछ उदाहरण हैं। आदिम तथा जनजातीय समाजों में अधिकांश कार्यों में प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है।
- अप्रत्यक्ष सहयोग-इस प्रकार का सहयोग द्वितीयक समूहों तथा आधुनिक जटिल समाजों की प्रमुख विशेषता है। इसमें व्यक्तियों द्वारा समान उद्देश्यों की पूर्ति असमान कार्यों के द्वारा की जाती। है अर्थात् एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक लोगों द्वारा अलग-अलग कार्य करना अप्रत्यक्ष सहयोग है। औद्योगिक क्षेत्र में, अंधिकारीतंत्र (नौकरशाही) में, अनुसंधान कार्यों में, अस्पतालों में तथा महाविद्यालयों आदि में पाया जाने वाला श्रम-विभाजन; इस प्रकार के सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं। आज अप्रत्यक्ष सहयोग का महत्त्व निरंतर बढ़ता जा रहा है।
(ब) ग्रीन (Green) द्वारा वर्गीकरण
एडब्ल्यू० ग्रीन ने सहयोग की प्रकृति, सामूहिक संगठन और दृष्टिकोण के आधार पर सहयोग को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया है-
- प्राथमिक सहयोग–इस प्रकार का सहयोग मुख्यतः प्राथमिक समूहों में पाया जाता है जिनमें व्यक्ति और समूह वास्तविक रूप से एकीभूत हो जाते हैं तथा जिनमें व्यक्ति, समूह और किए जाने वाले कार्य का पारस्परिक समीकरण (Identification) हो जाता है। इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति के स्वार्थ तथा समूह के स्वार्थ इतने अधिक हो जाते हैं कि उनके क्षेत्रों में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता। प्राथमिक सहयोग के उद्देश्य और साधन भी एक हो जाते हैं। और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा-समूह, मित्र-मंडली इत्यादि समूहों में प्रत्यक्ष व प्राथमिक सहयोग ही मुख्य रूप से पाया जाता है।
- द्वितीयक सहयोग–यह सहयोग द्वितीयक समूहों में पाया जाता है जो कि आधुनिक जटिल समाजों की प्रमुख विशेषता हैं। द्वितीयक सहयोग अत्यधिक विशिष्ट और औपचारिक होता है। इसमें लक्ष्य और साधन दोनों का बँटवारा होता है, परंतु संयुक्त रूप से नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करके दूसरों के कार्यों को सहायता पहुँचाता है। इस व्यक्ति की दृष्टि से हितप्रधान होता है क्योंकि व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही सहयोग प्रदान करता है। श्रम-विभाजन द्वितीयक सहयोग को प्रमुख उदहारण है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग कार्य करता हुआ भी दूसरों को सहयोग प्रदान करता है।
- तृतीयक सहयोग-ग्रीन के अनुसार, इस प्रकार के सहयोग में सहयोग करने वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण शुद्ध रूप से अवसरवादी होता है। इसकी प्रकृति अस्थिर होती है तथा सहयोग करने वालों में संगठन ढीला और शीघ्र टूट जाने वाला होता है। यह एक प्रकार से सहयोग न होकर अनुकूलन मात्र है क्योंकि इसमें लक्ष्य और साधनों का सामान्य प्रयत्नों द्वारा बँटवारा नहीं हो सकता। श्रमिकों एवं व्यवस्थापकों में सहयोग व संबंध इस श्रेणी का उदाहरण है।
(स) ऑगबर्न एवं निमकॉफ (Ogburn and Nimkoff) द्वारा वर्गीकरण
ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने सहयोग की निम्नलिखित तीन श्रेणियों का उल्लेख किया है-
- सामान्य सहयोग–इस प्रकार के सहयोग में अनेक व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हैं और एक-दूसरे को सहयोग देते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उदाहरण के लिए मजदूरों का ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अथवा किसी सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव के सम लोगों में जो सहयोग पाया जाता है, वह सामान्य सहयोग ही होता है।
- मित्रवत सहयोग-मित्रवत् सहयोग मुख्यत: आनन्द और सुख के लिए किया जाता है। मित्रों तथा संबंधियों के कार्यों में हाथ बँटाना इस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है क्योंकि ऐसा करने में व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है। इस प्रकार के सहयोग में स्वार्थ की मात्रा भी कुछ सीमा तक हो सकती है। सामूहिक नृत्य एवं गायन भी मित्रवत् सहयोग के ही उदाहरण हैं।।
- सहायक सहयोग–इस प्रकार के सहयोग में सहायता का तत्त्व प्रमुख होता है। जो बड़े-बड़े काम अकेले व्यक्तियों द्वारा नहीं हो सकते, उन्हें सामान्यत: सहायक सहयोग द्वारा ही पूरा किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक लोगों का मिलकर बाँध बनाना, पीड़ितों को सहायता प्रदान करना आदि सहायक सहयोग के ही उदाहरण हैं।
सहयोग का महत्त्व
सहयोग अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया है जिसके बिना हम सामाजिक जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। समाज का सारा ढाँचा, उसकी स्थिरता व निरंतरता सहयोग पर ही टिकी हुई होती है। सहयोग की आवश्यकता तथा महत्त्व को निम्नांकित क्षेत्रों में देखा जा सकता है-
- मनोवैज्ञानिक आवश्यकता-ग्रीन (Green) के अनुसार, सहयोग मनोवैज्ञानिक रूप से भी आवश्यक है। प्रारंभ से मुनष्य सहयोग करता आया है। स्त्री और पुरुष के सहयोग से बच्चा पैदा होता है। माता-पिता व अन्य सदस्यों द्वारा उसका पालन-पोषण किया जाता है और व्यक्तित्व को विकास किया जाता है। नवजात बालक बिना सहयोग के एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। अत: यह आवश्यक है कि माता-पिता व अन्य उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग दें।।
- समाजीकरण-समाजीकरण सीख की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। समाजीकरण सहयोग द्वारा ही संभव है। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में बच्चों के समाजीकरण में पाए जाने वाले सहयोग के कारण ही सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है। अतः समाजीकरण का मूलाधार भी सहयोग ही है।
- सामाजिक प्रगति प्रत्येक समाज में प्रगति के लिए सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सहयोग व्यक्तिगत हितों के स्थान पर समहूवाद की भावनाओं का विकास करता है और इस प्रकार सामूहिक प्रयासों द्वारा प्रगति को संभव बनाता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले अनुसंधान, जो कि सामाजिक प्रगति के लिए अनिवार्य हैं, सहयोग द्वारा ही संभव हो पाते हैं।
- आर्थिक महत्त्व-आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि समाज को आर्थिक ढाँचा सहयोग पर ही टिका होता है। अगर आर्थिक जगत में सहयोग न हो तो हमारी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकतीं।
- अन्य क्षेत्रों में महत्त्व-सहयोग का अनेक अन्य क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए युद्धकाल में बिना सहयोग के समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग का अपना अलग महत्त्व है। इसलिए यह कहा जाता है कि समाज का संपूर्ण ढाँचा सहयोग पर टिका हुआ है।
निष्कर्ष–उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सहयोग मानव जीवन की अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। समाज में कोई भी व्यक्तिगत यो सामूहिक लक्ष्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। अत: आज हम सहयोग के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते।
प्रश्न 4.
प्रतियोगिता किसे कहते हैं। इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए तथा समाज में इसका महत्त्व बताइए।
या
आधुनिक समाजों में प्रतियोगिता के आधारों एवं महत्त्व की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
प्रतियोगिता एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो कि आधुनिक समाजों की एक प्रमुख विशेषता बनती जा रही है। यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संघर्ष है क्योंकि इसमें सीमित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्ति या समूह एक साथ प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रतियोगिता को सीमित क्स्तुओं के आधिपत्य के लिए किया जाने वाला संघर्ष कहा जाता है। प्रतियोगिता एक ओर संघर्ष को कम करने का प्रयास है तो दूसरी ओर कई बार यह संघर्ष को बढ़ावा देने में भी सहायक प्रक्रिया है। सभी व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से सीमित वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। अत्यधिक प्रतियोगिता समाज में विघटन ला सकती है परंतु यह प्रतिभाओं के चयन और समाज की प्रगति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है। संघर्ष के विपरीत, प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं तथा इसमें सामान्यतः हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता है।
प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषाएँ
प्रतियोगिता को प्रमुख विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है-
- फैयरचाइल्ड (Fairchild) के अनुसार–(प्रतियोगिता सीमित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार के लिए किया जाने वाला संघर्ष है।”
- ग्रीन (Green) के अनुसार-“प्रतियोगिता में दो या अधिक व्यक्ति या समूह समान लक्ष्य को | प्राप्त करने का उपाय करते हैं जिसको कोई भी दूसरों के साथ बाँटने के लिए न तो तैयार होता | है और न ही इसकी अपेक्षा की जाती है।”
- बीसेंज एवं बीसेंज (Biesanz and Biesanz) के अनुसार-“प्रतियोगिता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य, जो कि इतना सीमित हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, को पाने के प्रयत्न को कहते हैं।”
- बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार-“प्रतियोगिता किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होड़ है, जो कि इतनी अपर्याप्त मात्रा में है जिससे माँग की पूर्ति नहीं की जा सकती।”
- सदरलैंड एवं सहयोगियों (Sutherland and Others) के अनुसार-“प्रतियोगिता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बीच उन संतुष्टियों, जिनकी पूर्ति सीमित होने के कारण सभी व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, को प्राप्त करने के लिए होने वाला अवैयक्तिक, अचेतन और निरंतर होने वाला संघर्ष है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतियोगिता दो या अधिक व्यक्तियों या समूहों में किसी सीमित वस्तु को प्राप्त करने के लिए होने वाला अचेतन, अवैयक्तिक और निरंतर संघर्ष है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाती है कि–
- प्रतियोगिता सामाजिक अंत:क्रिया का रूप है।
- यह एक विघटनकारी प्रक्रिया मानी जाती है।
- प्रतियोगिता तभी होती है जब साधन तो सीमित हैं परंतु उन्हें प्राप्त करने वाले अधिक हैं।
- प्रतियोगिता अप्रत्यक्ष संघर्ष का रूप है।
- यह व्यक्ति या समूह के अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है।
- यह उस परिस्थिति में भी होती है जबकि प्रतियोगी इस सीमित वस्तु को आपस में बाँटना नहीं चाहते हैं।
प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएँ
प्रतियोगिता के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों से इसकी अनेक विशेषताएँ भी स्पष्ट होती हैं जिनमें से प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- दो या अधिक व्यक्ति या समूह–प्रतियोगिता के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना जरूरी है। दो या अधिक पक्षों में सीमित साधनों को प्राप्त करने की होड़ को ही प्रतियोगिता कहते हैं।
- असहयोगी प्रक्रिया-प्रतियोगिता अंत:क्रिया का रूप होने के कारण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसे एक असहयोगी अथवा विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है।
- अचेतन प्रक्रिया–प्रतियोगितता को अचेतन सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसमें उन्हें प्रतिस्पर्धियों का न तो ज्ञान रहता है और न ही उनके द्वारा अपनाए जाने वाले प्रयत्नों के बारे में ही वे सचेत होते हैं। इसमें तो केवल उद्देश्य के प्रति ही चेतना पायी जाती है।
- अवैयक्तिक प्रक्रिया–प्रतियोगिता अचेतन प्रक्रिया होने के साथ एक अवैयक्तिक प्रक्रिया भी है। क्योंकि प्रतियोगी एक-दूसरे को नहीं जानते। सामान्यतः प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतियोगियों में (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर) सीधा संपर्क नहीं होता है। उदाहरण के लिए मेरठ विश्वविद्यालय की बी०ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने वाले हजारों प्राथी एक-दूसरे को न जानते हुए भी दूसरों से अधिक अंक प्राप्त करने लिए प्रयत्नशील होते हैं।
- निरंतर होने वाली प्रक्रिया-प्रतियोगिता संघर्ष के विपरीत निरंतर होने वाली प्रक्रिया है क्योंकि यह कभी रुकती नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण रूप में अपनी भूमिका निभाती रहती है। जीवन का एक भी पक्ष इससे अछूता नहीं है।
- सार्वभौमिक प्रक्रिया–प्रतियोगिता एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योकि यह सभी देशों में तथा सभी कालों में किसी-न-किसी रूप में विद्यमान रहती है। आज के आधुनिक समाजों में तो यह प्रायः सभी समाजों में तथा समाज के सभी पक्षों में देखी जा सकती है।
प्रतियोगिता की परिभाषाओं तथा विशेषताओं से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास है जो इतना सीमित है कि सभी प्रतियोगी उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तव में, इसी संदर्भ में बीसेज एवं बीसेज (Biesanz and Biesanz) ने जो परिभाषा दी है वह पूरी तरह से प्रतियोगिता का अर्थ स्पष्टं करती हैं। उनके अनुसार, प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी एक ही वस्तु को प्राप्त करने लिए किए गए प्रयास को कहते हैं जो इतनी सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं हो सकते।”
प्रतियोगिता के प्रमुख स्वरूप
प्रतियोगिता एक सार्वभौमिक, निरंतर, वैयक्तिक तथा अचेतन रूप में होने वाली प्रक्रिया है। इसके अनेक प्रकार या स्वरूप हैं जिनमें से प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं-
(अ) गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) ने प्रतियोगिता के चार प्रमुख स्वरूप बताए हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है-
- आर्थिक प्रतियोगिता–आर्थिक प्रतिस्पर्धा आज के युग में सर्वाधिक व्यापक प्रतियोगिता है। व्यापारियों और उद्योगपतियों में यह प्रतियोगिता देखी जा सकती है। वस्तुओं की माँग जितनी अधिक होती है उतनी ही प्रतियोगिता अधिक होती है। यह उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनिमय जैसे पक्षों में पायी जाती है।
- सांस्कृतिक प्रतियोगिता-जब दो संस्कृतियाँ परस्पर संपर्क में आती हैं तो उनमें विविध प्रकार की प्रतियोगिता विकसित होती है। प्रत्येक संस्कृति अपने तत्त्वों को श्रेष्ठ मानकर उसे दूसरों पर थोपने का प्रयास करती है। कई बार सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा सांस्कृतिक संघर्ष में बदल जाती है। मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों, व्यवसाय के तरीकों तथा विभिन्न संस्थाओं में पायी जाने वाली प्रतियोगिता सांस्कृतिक प्रतियोगिता ही कही जाती है।
- भूमिका या स्थिति के लिए प्रतियोगिता–गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, प्रतियोगिता को तीसरा स्वरू। भूमिका या स्थिति के होने वाली होड़ है। प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह उन भूमिकाओं को करना चाहता है जो अन्य भूमिकाओं से महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी प्रकार उच्च सामाजिक स्थिति के लिए भी होड़ पायी जाती है। कला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रतियोगिता देखी जा सकती है।
- प्रजातीय प्रतियोगिता–एक प्रजाति दूसरी प्रजातियों से शारीरिक लक्षणों एवं अन्य क्षमताओं की दृष्टि से भिन्न होती है। कई उपजातियाँ अपने को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती हैं। यह श्रेष्ठता या निम्नता का भाव विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिता को जन्म देता है। प्रजातीय प्रतियोगिता ही कई बार प्रजातीय संघर्ष का रूप ग्रहण कर लेती है।
(ब) अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएँ-गिलिन एवं गिलिन ने उपर्युक्त केवल चार प्रकार की प्रतियोगिता का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्वरूप भी हैं जिनमें से प्रमुख स्वरूप अग्रलिखित हैं-
- वैयक्तिक प्रतियोगिता–इसे चेतन प्रतियोगिता भी कहते हैं तथा इसमें प्रतियोगी एक-दूसरे को जानते हैं। उदाहरणार्थ-खेल जगत में पायी जाने वाली प्रतियोगिता वैयक्तिक प्रतियोगिता होती है क्योंकि इसमें प्रतियोगी एक-दूसरे को भली-भाँति जानते हैं।
- अवैयक्तिक प्रतियोगिता-इसे अचेतन प्रतियोगिता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी एक-दूसरे को नहीं जानते तथा उनमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। परीक्षाओं में बैठने वाले हजारों परीक्षार्थियों के मध्य प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिता का प्रमुख उदाहरण है क्योंकि वे अचेतन रूप में अन्य परीक्षार्थियों की तुलना में आगे निकलने का प्रयास करते हैं।
- जातीय प्रतियोगिता–भारत में परंपरागत रूप से विभिन्न जातियाँ प्रकार्यात्मक संबंधों द्वारा एक-दूसरे से बँधी हुई थी परंतु आज नौकरियों को प्राप्त करने या समाज में प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त करने में विभिन्न जातियों में प्रतियोगिता देखी जा सकती है।
- राजनीतिक प्रतियोगिता–विभिन्न नेता तथा राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के एक-दूसरे से राजनीतिक प्रतियोगिता करते हैं। प्रत्येक दल का नेता अपनी एक निश्चित स्थिति बनाना चाहता है ताकि चुनाव के समय वह इसका लाभ उठा सके।
- धार्मिक प्रतियोगिता–प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अपने को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ मानता है और इसका प्रचार व प्रसार भी करता है। धार्मिक प्रतियोगिता अगर घृणित भावनाओं के आधार पर होने लगती है तो सांप्रदायिक दंगे तक उभर सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता-आज संसार के विभिन्न देशों में आर्थिक तथा सैनिक क्षेत्रों में प्रतियोगिता स्पष्टतः देखी जा सकती है क्योंकि प्रत्येक देश अन्य देशों की तुलना में आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से आगे निकलने का प्रयास करता है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता संघर्ष का कारण भी बन जाती है।
प्रतियोगिता के आधार
गिलिन एवं गिलिन ने प्रतियोगिता के दो प्रमुख आधार अथवा निर्धारक कारक बताए हैं जो कि निम्नलिखित हैं-
- मूल्यों की व्यवस्था तथा
- समूह की संरचना।
किसी भी समाज या समूहों में पाए जाने वाले मूल्यों की व्यवस्था ही यह निर्धारिण करती है कि अंत:क्रिया का स्वरूप सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष आदि में से किस प्रकार का होगा। अगर व्यक्तिवाद पर आधारित भौतिकवादी मूल्ये व्यवस्था किसी समाज में है तो वहाँ प्रतियोगिता अधिक पायी जाती है। अगर आध्यात्मिक संस्कृति है तो प्रतियोगिता की मात्रा कम होती है। सामूहिक जीवन से संबंधित मूल्यों की व्यवस्था का प्रतियोगिता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
मूल्यों की व्यवस्था के साथ-साथ समूह की संरचना भी प्रतियोगिता की मात्रा को निर्धारित करती है। अगर कोई समाज या समूह बंद है तो उनमें प्रतियोगिता को संस्थागत रूप से नियंत्रित कर लिया जाता है। अगर समाज या समूह खुले प्रकार का है तो ऐसी संरचना स्वयं प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने वाली होती है। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से प्रतियोगिता का अभाव इसकी बंद सामाजिक संरचना का ही परिणाम माना जाता है। साथ ही पश्चिमी समाजों में तथा आज भारत में अत्यधिक प्रतियोगिता, खुली सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। अगर संरचना प्रतियोगिता के अवसर ही प्रदान नहीं करती तो प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती और अगर प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देने वाली संरचना है तो सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता देखी जा सकती है।
प्रतियोगिता का महत्त्व तथा परिणाम
प्रतियोगिता यद्यपि एक असहयोगी प्रक्रिया मानी जाती है फिर भी यह परिणामों की दृष्टि से सदैव विघटनकारी नहीं होती अपितु समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतियोगिता, योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया है। अगर व्यक्ति को पता हो कि उसे उद्देश्य पूर्ति के लिए अनेक अन्य लोगों से प्रतियोगिता करनी है है तो वह अपनी योग्यता और कुशलता में पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। प्रतियोगिता सामाजिक चुनाव की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करना संभव हो जाता है। गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) ने इस प्रक्रिया के विविध परिणामों का उल्लेख किया है जिससे इसका महत्त्व स्पष्ट होता है। इसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं-
- सहयोगात्मक परिणाम-अगर किसी समाज में स्वस्थ प्रतियोगिता पायी जाती है तो संगठनात्मक दृष्टि से इसके अच्छे परिणाम निकलते हैं क्योंकि इससे प्रत्येक व्यवसाय में अच्छे लोगों को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है। प्रतियोगिता के कारण अनेक व्यावसायिक संगठनों का भी विकास होता है जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं। गिलिने एवं गिलिन ने इसी दृष्टि से प्रतियोगिता जैसी असहयोगी प्रक्रिया को सहयोगी प्रक्रिया कहा है।
- असहयोगात्मक परिणाम-कई बार, बल्कि, बहुधा, प्रतियोगिता बड़ा कटु रूप धारण कर लेती है क्योंकि प्रतियोगी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी नियमों को तोड़कर अवैधानिक साधन अपनाने लगते हैं। कई बार यह कटुता इतनी अधिक हो जाती है कि प्रतिद्वंद्वियों में संघर्ष तक हो जाता है। इसी दृष्टि से इसके असहयोगी परिणामों की विवेचना की जाती है।
- व्यक्तित्व संबंधी परिणाम-अगर समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर प्रतियोगिता होती है तो यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता प्रदान करती है। प्रतियोगिता में लगे व्यक्ति अन्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे उनका दृष्टिकोण विस्तृत बनता है, बोध शक्ति बढ़ती है और सहानुभूति की भावना गहरी होती है। ये सभी बातें व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहन देती हैं।
- प्रगति संबंधी परिणाम-गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, प्रतियोगिता के प्रगति संबंधी परिणाम भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। एक तो प्रतियोगिता परिवर्तित परिस्थितियों में समायोजन में सहायता देती है तो दूसरी ओर यह व्यक्ति को नवीन तरीके खोजने तथा अपने कार्य को अत्यधिक उत्तम तरीके से करने के लिए प्रेरणा देती है। प्रतियोगिता आविष्कारों की भी जननी है। तथा इसीलिए यह विधि प्रकार से समाज की प्रगति में सहायता प्रदान करती है।
- सामूहिक दृढ़ता संबंधी परिणाम–प्रतियोगिता सामूहिक एकता तथा दृढ़ता की दृष्टि से भी हत्त्वपूर्ण है क्योंकि नियमों के भीतर स्वस्थ प्रतियोगिता योग्यतानुसार कार्य करने की प्रेरित करती है तथा इसका अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती है क्योंकि उचित ढंग से कार्य करने पर समूह की एकता बनी रहती है। प्रतियोगिता समूह की एकता के लिए तभी खतरा बन सकती है जबकि प्रतियोगिता अव्यवस्थित व नियम-विहीन हो जाती है और घृणा तथा संघर्ष का रूप ले लेती है।
- विघटन-संबंधी परिणाम-गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, प्रतियोगिता सामाजिक विघटन के लिए भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी है। प्रतियोगिता आविष्कारों को प्रोत्साहन देती है और कई बार व्यक्ति इन आविष्कारों के कारण उत्पन्न परिवर्तन से अनुकूलन नहीं रख पाते। ऐसी नवीन परिस्थिति में सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि इसमें असामंजस्य की स्थिति विकसित हो जाती है। सामाजिक एकता की बजाय सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन देकर यह अपनी असहयोगी भूमिका निभाती है।
निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतियोगिता समाज के लिए प्रकार्यात्मक ही नहीं है अपितु यह व्यक्ति और समूह की दृष्टि से प्रकार्यात्मक है और इसी दृष्टि से यह एक संगठनात्मक प्रक्रिया भी है। प्रतियोगिता कार्यों को अच्छी प्रकार से करने की प्रेरिणा देती है, यह महत्त्वकांक्षाओं में वृद्धि करती है तथा प्रतिद्वंद्वी की चुनौती को स्वीकार कर अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्रदान करती है। अतः स्वस्थ एवं नियंत्रित प्रतियोगिता को कम विघटनकारी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। यह विघटनकारी तभी कही जाती है जबकि यह अनियंत्रित हो जाती है और प्रतियोगिता में घृणा और हिंसा की भावना आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में प्रतियोगिता हिंसा तथा संघर्ष में भी बदल जाती है और समाज, समूह तथा व्यक्ति के लिए विघटनकारी हो जाती है। अतः यह दोनों प्रकार की प्रक्रिया है तथा समाज में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है।
प्रश्न 5.
संघर्ष किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकार बताइए।
या
संघर्ष को परिभाषित कीजिए तथा समाज में इसका महत्व समझाइए।
या
संघर्ष क्या है? इसके कारणों की विवेचना कीजिए।
या
संघर्ष से आप क्या समझते हैं? संघर्ष एवं सहयोग तथा संघर्ष एवं प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
सहयोग की तरह संघर्ष भी सामाजिक जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सहयोग को एक प्रमुख सहयोगी प्रक्रिया माना जाता है, जबकि संघर्ष को एक प्रमुख असहयोगी प्रक्रिया माना जाता है। सहयोग और संघर्ष को अधिकतर लोग एक-दूसरे की विरोधी प्रक्रियाएँ मानते हैं, जबकि इनको विरोधी न कहकर एक-दूसरे की परक एवं सहगामी प्रक्रियाएँ कहना अधिक उचित है। इसका कारण यह है कि सहयोग के बिना संघर्ष के बिना सहयोग की कल्पना केवल सैद्धांतिक रूप में ही की जा सकती है। यह एक ऐसी असहयोगी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिद्वंद्वी समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा तक का सहारा लेते हैं। वास्तव में यह दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक रोकने का प्रयास है।
संघर्ष का अर्थ एवं परिभाषाएँ
संघर्ष को प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है-
फेयरचाइल्ड (Fairchild) के अनुसार-“संघर्ष एक प्रक्रिया या परिस्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक-दूसरे के उद्देश्यों को क्षति पहुँचाते हैं, एक-दूसरे के हितों की संतुष्टि पर रोक लगाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए दूसरों को चोट पहुँचानी पड़े या नष्ट करना पड़े।
ग्रीन (Green) के अनुसार–“संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करना, रोकना तथा उसे बलपूर्वक रोकने के प्रयास को कहते हैं।”
पार्क एवं बर्गेस (Park and Burgess) के अनुसार-“संघर्ष और प्रतियोगिता विरोध के दो रूप हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा सतत एवं अवैयक्तिक होती है, जबकि संघर्ष का रूप असतत वे वैयक्तिक होता है।”
फिचर (Fichter) के अनुसार--‘संघर्ष पारस्परिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक-दूसरे को दूर रखने का प्रयास करते हैं।”
गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार-“संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति विरोधी की हिंसा या हिंसा के भय के द्वारा करते हैं।”
कोजर (Coser) के अनुसार–‘स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले संघर्ष को ही सामाजिक संघर्ष कहा जाता है जिनमें विरोधी दलों का उद्देश्य अपने प्रतिस्पर्धी को प्रभावहीन करना, हानि पहुँचाना अथवा समाप्त करना भी है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा का प्रयोग करके या हिंसा का भय देकर करते हैं। यह प्रत्यक्ष और चेतन प्रक्रिया है जिसमें सामान्यत: दूसरे पक्ष को किसी-न-किसी प्रकार की हानि पहुँचाने का प्रयास किया जाता है।
संघर्ष की प्रमुख विशेषताएँ
संघर्ष के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों से इसकी प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
- सामाजिक प्रक्रिया-संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए दो व्यक्तियों अथवा समूहों का होना जरूरी है। यह एक प्रमुख असहयोगी प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में किसी-न-किसी रूप में पायी जाती है।।
- हिंसा या धमकी का प्रयोग-संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष दूसरे के हितों को नुकसान पहुँचाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है अथवा ऐसा करने की धमकी देता है।
- चेतन प्रक्रिया-संघर्ष को एक चेतन प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ विरोधी के हितों को नुकसान पहुँचाना या उसे समाप्त कर देने का भी प्रयास किया जाता है।
- वैयक्तिक प्रक्रिया-संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति या समूह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संघर्ष करते हैं। जब एक समूह दूसरे से संघर्ष करता है तो यह प्रतिद्वंद्वियों पर केंद्रित न होकर समूह विशेष पर केंद्रित होता है।
- अनिरंतर प्रक्रिया संघर्ष अनिरंतर होने वाली प्रक्रिया है अर्थात् संघर्ष निरंतर न होकर रुक-रुककर होता रहता है। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सदैव संघर्षरत नहीं रह सकता। उसे कुछ समय बाद पुन: अपनी शक्ति संचित करनी पड़ती है।
- सार्वभौमिक प्रक्रिया संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि यह प्रत्येक समाज में किसी-न-किसी रूप में पायी जाती है। यह सामाजिक जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।
संघर्ष के विभिन्न स्वरूप
संघर्ष अनेक प्रकार का होता है। इसे विद्वानों ने अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है। इस संबंध में प्रमुख विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं-
(अ) मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) द्वारा वर्गीकरण मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है1. प्रत्यक्ष संघर्ष-प्रत्यक्ष संघर्ष दो पक्षों में आमने-सामने होने वाला संघर्ष है। इस प्रकार के संघर्ष को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि प्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण हैं।
2. अप्रत्यक्ष संघर्ष—इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति या समूह आमने-सामने नहीं आते हैं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से संघर्ष करते हैं। इस प्रकार के संघर्ष में विरोधी के प्रति घृणा, अविश्वास तथा शत्रुता की भावनाएँ पायी जाती हैं। असीमित प्रतिस्पर्धा तथा शीत युद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं।
( अ ) किंग्सले डेविस (Kingsley Davis) द्वारा वर्गीकरण
किंग्सले डेविस ने भी संघर्ष को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है
- आंशिक संघर्ष-यह कम मात्रा में पाया जाने वाला संघर्ष होता है। जब दो समूहों में लक्ष्यों के बारे में तो सहमति हो परंतु उनको प्राप्त करने के साधनों के बारे में मतभेद हो जाए तो इसे आंशिक संघर्ष कहते हैं।
- पूर्ण संघर्ष—इस प्रकार के संघर्ष में विभिन्न संघर्षरत समूहों में न तो उद्देश्यों (लक्ष्यों) के बारे में और न ही इन्हें प्राप्त करने के बारे में सहमति होती है। उद्देश्यों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन, ऐसी स्थिति में, बल प्रयोग द्वारा अथवा इसकी धमकी द्वारा रह जाता है। आंशिक और पूर्ण संघर्ष में अंतर केवल अंशों का है।
(स) गिलिन एवं गिलिन (Gilin and Gillin) द्वारा वगीकरण, गिलिन एवं गिलिन ने संघर्ष को प्रमुख पाँच प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है जो कि निम्नलिखित हैं-
- वैयक्तिक संघर्ष-वैयक्तिक संघर्ष में दो व्यक्तियों के हितों में टकराव होने के फलस्वरूप उत्पन्न संघर्ष को सम्मिलित किया जाता है। वैयक्तिक संघर्ष प्रत्यक्ष संघर्ष होता है जिसमें दोनों पक्षों में गाली-गलौज, मार-पीट या घृणा के भाव सम्मिलित होते हैं। यह मुख्यत: स्त्री, धन या जमीन को लेकर होता है।
- प्रजातीय संघर्ष–प्रजाति सामान्य शारीरिक लक्षणों वाला एक समूह है। इन्हीं शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति अपने को दूसरी प्रजाति से भिन्न समझती है तथा इसी आधार पर उनमें श्रेष्ठता या निम्नता के भाव भी विकसित होते हैं। यह भाव एवं अंतर दोनों में कई बार संघर्ष के कारण भी बन जाते हैं। अमेरिका में सफेदपोश और नीग्रो प्रजातियों में संघर्ष प्रजातीय संघर्ष के प्रमुख उदाहरण है। प्रजातीय श्रेष्ठता के आधार पर शोषण भी किया जाता है।
- वर्ग संघर्ष–वर्ग आधुनिक समाजों का प्रमुख लक्षण है। यद्यपि इसका प्रमुख आधार आर्थिक है। | फिर भी यह सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक हितों तथा प्रतिष्ठा से भी जुड़ा होता है। विभिन्न वर्ग हितों में विरोधाभास के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करने लगते हैं। पूँजीपति तथा श्रमिक वर्ग में पाए जाने वाले संघर्ष इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
- राजनीतिक संघर्ष–राजनीतिक संघर्ष भी वर्तमान युग की देन है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आए दिन संघर्ष देखे जा सकते हैं। राजनीतिक दलों में उद्देश्यों के टकराव के कारण होने वाला अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संघर्ष भी राजनीतिक संघर्ष का एक उदाहरण है। विश्व के दो विभिन्न राष्ट्रों में होने वाले संघर्ष को भी राजनीतिक संघर्ष कहते हैं जिसमें हजारों, लाखों लोगों की जाने जा सकती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष-संघर्ष स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं होते, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे जा सकते हैं। आज सभी राष्ट्र कई गुटों में विभाजित हैं। इन गुटों में भी विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टकराव की स्थिति बनी रहती है। आज दो राष्ट्रों में होने वाला संघर्ष केवल उन्हीं राष्ट्रों तक सीमित नहीं रहता, अपितु अनेक अन्य राष्ट्र भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में सहायता देते हैं।
उपर्युक्त संघर्ष के प्रकारों के अतिरिक्त कई बार पारिवारिक संघर्ष, सामुदायिक संघर्ष, जातीय व उपजातीय संघर्ष, धार्मिक एवं सांप्रदायिक संघर्ष का भी उल्लेख किया जा सकता है।
संघर्ष के प्रमुख कारण
संघर्ष का कोई एक कारण नहीं है, अपितु यह अनेक कारणों से होते हैं। वास्तव में, संघर्ष के विभिन्न स्वरूपों से ही इसके कारणों का पता चल जाता है। गिलिन एवं गिलिन ने इसके प्रमुख कारणों को चारै श्रेणियों में विभाजित किया है–
- व्यक्तिगत भिन्नताएँ-व्यक्तिगत, भिन्नताएँ, वैयक्तिक संघर्ष तथा सामूहिक संघर्ष को जन्म | देती हैं। व्यक्तिगत मनोवृत्तियों, मूल्यों आदतों, क्षमताओं, दृष्टिकोणों तथा स्वभाव में अंतर अनेक परिस्थितियों में संघर्ष का कारण बन जाता है।
- सांस्कृतिक भिन्नताएँ–सांस्कृतिक भिन्नताओं का संबंध विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में पाए जाने वाले अंतर से है। संस्कृति के आधार पर भी राष्ट्रों में श्रेष्ठता या भिन्नता की भावना पायी जा सकती है। विभिन्न प्रजातियों, जातियों, वर्गों या राष्ट्रों में सांस्कृतिक भिन्नताओं के आधार पर संघर्ष पैदा होते रहते हैं।
- परस्पर विरोधी हितों या स्वार्थों का टकराव-परस्पर विरोधी हिंतों व स्वार्थों का टकराव | वैयक्तिक, सामूहिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय किसी भी स्तर पर हो सकता है। पूँजीपतियों तथा श्रमिकों में पाए जाने वाले संघर्ष का प्रमुख कारण परस्पर विरोधी हितों का पाया जाना ‘तथा इनमें टकराव ही है।
- सामाजिक परिवर्तन—यह भी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। किसी भी समाज के विभिन्न समूहों में परिवर्तन एक समान गति से नहीं होता है। अगर एक समूह परिवर्तन के परिणामस्वरूप आधुनिकीकृत हो जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है तो उनमें मूल्यों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न पीढ़ियों में पाया जाने वाला संघर्ष भी सामाजिक परिवर्तन की ही देन है।
संघर्ष का महत्त्व
यद्यपि संघर्ष एक असहयोगी व विघटनकारी प्रक्रिया है फिर भी यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है। जिसका जीवन में अपना अलग महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज तो प्रकार्यवादी विद्वान् भी इसके प्रकार्यात्मक महत्त्व को स्वीकार करने लगे हैं। इसके महत्त्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है-
- चेतना का विकास संघर्ष मानवीय चेतना का प्रमुख आधार है क्योंकि इसी से व्यक्ति में अपने प्रति, समूह के प्रति अथवा राष्ट्र के प्रति चेतना की भावना का विकास होता है। रयूटर एवं हार्ट (Reuter and Hart) ने इस संदर्भ में लिखा है-“संघर्ष समस्त चेतन जीवन का आधार है। आत्म-चेतना तथा सामूहिक चेतना संघर्ष के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है।”
- व्यक्तित्व का निर्माण–संघर्ष व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक है क्योंकि अगर व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष न करें तो वे न तो पर्यावरण से अनुकूलन ही कर सकते हैं और न ही वे अपनी आंतरिक क्षमता का विकास ही कर सकते हैं।
- एकीकरण को बढ़ावा-संघर्ष को एक दृष्टि से प्रकार्यात्मक माना जाता है कि यह एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अगर बाहरी समूह में संघर्ष होता है तो समूह के सदस्यों में | आंतरिक एकीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है।
- मानव जीवन का संगठन संघर्ष मानव जीवन को संगठित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघर्षों का सामना करने के लिए मानव अपनी आंतरिक शक्ति का पूर्ण विकास करते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन के कारण ही व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का सरलता से सामना कर लेता है।
उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघर्ष एक प्रमुख असहयोगी प्रक्रिया है। परन्तु संघर्ष एक विघटनकारी प्रक्रिया होते हुए भी समाज की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। मैकाइवर एवं पेज ने इस दृष्टि से उचित ही कहा है कि संघर्ष के द्वारा ही सहयोग की भावना का विकास होता है।
सहयोग एवं संघर्ष में अंतर
सहयोग और संघर्ष दोनों सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं तथा सामाजिक जीवन की अभिन्न प्रक्रियाएँ होने के नाते एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों में पाए जाने वाले प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं-
प्रतियोगिता और संघर्ष में भेद
प्रतियोगिता और संघर्ष को आधुनिक समाजों में पायी जाने वाली दो प्रमुख सहयोगी प्रक्रियाएँ माना गया। है। यद्यपि संघर्ष परंपरागत समाजों में भी पाया जाता था परंतु इसकी मात्रा कहीं कम थी। प्रतियोगिता और संघर्ष दोनों एक नहीं हैं अपितु इनकी प्रकृति में काफी अंतर पाया जाता है। पार्क एलं बर्गेस (Park and Burgess) ने लिखा है-“संघर्ष और प्रतियोगिता विरोध के दो रूप हैं। जिनमें प्रतियोगिता सतत और अवैयक्तिक होती है, जबकि संघर्ष का रूप अनिरंतर और वैयक्तिक होता है। दोनों में निम्नलखित प्रमुख अंतर पाए जाते हैं-
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाती है कि प्रतियोगिता और संघर्ष दोनों असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं परंतु दोनों की प्रकृति में काफी अंतर पाया जाता है।
प्रश्न 6.
सामाजिक स्तरीकरण क्या है? भारतीय समाज के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए।
या
सामाजिक स्तरीकरण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
सामाजिक स्तरीकरण (संस्तरण) एवं सामाजिक गतिशीलता ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रियाएँ हैं जो किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक समाज में पायी जाती हैं। आपने देखा होगा कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी जाति तथा एक निश्चित आय वाले समूह, जिसे वर्ग कहा जाता है, का सदस्य है। विभिन्न जातियों एवं वर्गों को सामाजिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। इनमें एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है। इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि इसी के आधार पर समाज में तनाव तथा विरोध विकसित होते हैं। इसी के अध्ययन से हमें पता चलता है कि किसी समाज के व्यक्तियों को उपलब्ध जीवन अवसरों, सामाजिक प्रस्थिति एवं राजनीतिक प्रभाव में कितनी असमानता है।
स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएँ
सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन है। इन स्तरों में ऊँच-नीच या संस्तरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्तियों या समूहों को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा एवं जीवन अवसर उपलब्ध होते हैं, जबकि इससे निम्न स्थिति वाले व्यक्तियों या समूहों को ये सब कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार, समाज के विभिन्न समूहों में पायी जाने वाली आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक असमानता को ही स्तरीकरण कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्यों और समूहों को प्रस्थिति के पदानुक्रम में न्यूनाधिक स्थायी रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है। यह एक दीर्घकालीन उद्देश्य वाली सचेतन प्रक्रिया है। समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक स्तरीकरण को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-
जिस्बर्ट (Gisbert) के अनुसार-“सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसी स्थायी श्रेणियों तथा समूहों में बाँटने की व्यवस्था से है जो कि उच्चता एवं अधीनता के संबंधों से परस्पर संबद्ध होते हैं। इस परिभाषा में उच्चता एवं अधीनता के आधार पर समूह को विभाजित किया जाना ही स्तरीकरण माना गया है। इसमें दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं—प्रथम, यह किस जिस आधार से समूह को स्तरीकृत किया जाता है वह स्थिर रहती है, तथा द्वितीय, उच्चता तथा निम्नता के आधार पर विभिन्न समूह प्रतिष्ठित होते हैं और वे परस्पर संबंध रखते हुए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं।
सदरलैण्ड एवं वुडवर्ड (Sutherland and Woodward) के अनुसार-“साधारणतः स्तरीकरण अंत:क्रिया अथवा विभेदीकरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि स्तरीकरण का आधार प्रस्थिति है। समाज को प्रस्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुँच के आधार पर समाज में समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। इसकी तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। समाज को एक ऐसे अधिक्रम के रूप में देखा जाता है जिसमें कई परतें शामिल हैं। इस अधिक्रम में अधिक सुविधापात्र शीर्ष पर तथा कम सुविधापात्र तल के निकट हैं।
भारतीय समाज में स्तरीकरण के उदाहरण
भारतीय समाज में जब हम अपने आस-पड़ोस का प्रेक्षण करते हैं तो हमें जाति के आधार पर ऊँच-नीच दिखाई देती है। जाति पर आधारित स्तरीकरण की व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म पर आधारित होती है। विभिन्न जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठता में अंतर होता है तथा उनमें ऊँच-नीच के आधार पर खान-पान, विवाह, सामाजिक सहवास इत्यादि पर भी प्रतिबन्ध पाए जाते हैं। परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था। अस्पृश्यता से जाति व्यवस्था में पायी जाने वाली ऊँच-नीच का पता चलता है। अस्पृश्य जातियों को अपवित्र माना जाता था तथा उनसे अन्य जातियाँ दूरी बनाए रखती थीं। समकालीन भारतीय समाज में यद्यपि जाति व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं, तथापि जातिगत भेदभाव आज भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं।
भारत में समाजिक स्तरीकरण का दूसरा आधार, आर्थिक आधार पर निर्मित होने वाले वर्ग हैं। भू-पति एवं कारखानों के मालिक भूमिहीन एवं श्रमिक वर्ग से कहीं अधिक सुविधा संपन्न होते हैं तथा विविध रूपों में अधीनस्थ वर्गों का शोषण करते हैं। बहुत-से विद्वान् अब यह मानने लगे हैं कि जातिगत भेदभाव के साथ-साथ भारत में आर्थिक आधार पर ऊँच-नीच भी अधिक हो गई है। इसीलिए आस-पड़ोस में रहने वाले अनेक परिवार न केवल अन्य जातियों के अपितु हमसे अधिक अमीर या गरीब भी हो सकते हैं।
प्रश्न 7.
सामाजिक वर्ग क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
या
सामाजिक स्तरीकरण के एक स्वरूप के रूप में वर्ग व्यवस्था की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
जाति तथा वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं। जाति से अभिप्राय एक ऐसे. समूह से है जिसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्म से मिलती है तथा जीवन-पर्यंत वह इस सदस्यता को नहीं बदल सकता। वर्ग एक खुली व्यवस्था है जिसकी सदस्यता व्यक्ति को उसकी योग्यता व गुणों के आधार पर मिलती है तथा वह इसे परिवर्तित कर सकता है। अमेरिका तथा पश्चिमी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख रूप वर्गीय स्तरीकरण ही है। भारत में जैसे-जैसे आर्थिक आधार पर सामाजिक स्तरों का निर्माण हो रहा है तथा चेतना में वृद्धि होती जा रही है, वैसे-वैसे वर्ग व्यवस्था विकसित होने लगी है।
सामाजिक वर्ग का अर्थ एवं परिभाषाएँ
जब एक ही सामाजिक स्थिति के व्यक्ति समान संस्कृति के बीच रहते हैं तो वे एक सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह हैं जिनकी सामाजिक स्थिति लगभग समान हो और जो एक-सी ही सामाजिक दशाओं में रहते हों। एक वर्ग के सदस्य एक जैसी सुविधाओं का उपभोग करते हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। एक-सी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के व्यक्तियों को एक वर्ग विशेष का नाम दे दिया जाता है; जैसे-पूँजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि। प्रमुख विद्वानों ने सामाजिक वर्ग की परिभाषाएँ इस प्रकार से दी हैं-
मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार-“एक सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भी भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से भिन्न है।’ लेपियर (LaPiere) के अनुसार-“एक सामाजिक वर्ग सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह है जिसको संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थान अथवा पद प्रदान किया जाता है।”
ऑगबर्न एवं निमकॉफ (Ogburn and Nimkoff) के अनुसार–“सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक योग है जिनका किसी समाज में निश्चित रूप से एक समान स्तर होता है।”
क्यूबर (Cuber) के अनुसार-“एक सामाजिक वर्ग अथवा सामाजिक स्तर जनसंख्या का एक बड़ा भाग अथवा श्रेणी है जिसमें सदस्यों का एक ही पद अथवा श्रेणी होती है।”
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक वर्ग लगभग समान स्थिति वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य समूह के प्रति जागरूक हैं। विभिन्न वर्गों की सामाजिक स्थिति भिन्न होती है।
सामाजिक वर्ग की प्रमुख विशेषताएँ
सामाजिक वर्ग की परिभाषाओं से इसकी अनेक मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं-
- निश्चित संस्तरण-वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति कुछ श्रेणियों में विभाजित होते हैं। यद्यपि वर्गों की संख्या के बारे में विद्वानों में सहमति नहीं है। फिर भी यह निश्चित है कि कुछ वर्गों का स्थान ऊँचा और कुछ का नीचा होता है।
- हर्र की सर्वव्यापकता-वर्ग मानव समाज की एक सर्वव्यापी प्रघटना है। मार्क्स के अनुसार, वर्ग व्यवस्था प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल में भी किसी-न-किसी रूप में सदैव विद्यमान रही है। यद्यपि इन्होंने वर्गविहीन समाज की कल्पना की थी, परंतु अधिकांश विद्वान् वर्गविहीन समाज को केवल एक दिवास्वप्न मानते हैं क्योंकि मानव जीवन के इतिहास में इसकी उपलब्धि संभव नहीं है।
- वर्ग चेतना-वर्ग चेतना के कारण वर्ग विशेष के सदस्यों में समानता की भावना प्रोत्साहित होती है व उस वर्ग को स्थायित्व प्राप्त होता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना को वर्ग के निर्माण की एक अनिवार्य विशेषता माना है क्योंकि केवल समान आर्थिक स्थिति ही वर्ग के निर्धारण में पर्याप्त नहीं है।
- अर्जित सदस्यता-वर्ग की सदस्यता जन्म द्वारा नहीं वरन् योग्यता और कुशलता द्वारा अर्जित होती है। व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता से वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति, जो निम्न वर्ग का सदस्य है, प्रयत्न करने से उच्च वर्ग का सदस्य बन सकता है। ठीक उसी प्रकार, एक उच्च वर्ग का सदस्य अपनी अयोग्यता के कारण निम्न वर्ग का सदस्य बन्न सकता है।
- मुक्त व्यवस्था-वर्ग जाति के समान बंद व्यवस्था न होकर मुक्त व्यवस्था है। किसी व्यक्ति का वर्ग उसकी परिस्थिति के अनुसार परिर्वितत भी हो सकता है। इसी गतिशीलता के कारण इसे मुक्त व्यवस्था कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलथ्ध हैं जिससे कि वह अपने गुणों, योग्यता तथा क्षमता के आधार पर उच्च वर्ग का सदस्य बन सके। उदाहरण के लिए एक सामान्य श्रमिक अपनी मेहनत, लगन व योग्यता से उसी फैक्ट्री का संचालक तक बन सकता है। जिसमें कि वह काम करता है।
- सीमित सामाजिक संबंध–प्रत्येक वर्ग के समुदाय अपने ही वर्ग के सदस्यों से संबंध रखते हैं। सामान्यतः उच्च वर्ग के सदस्य निम्न वर्ग के सदस्यों से संबंध स्थापित करने में सम्मान की हानि समझते हैं अर्थात् उनमें उच्चता की भावना होती है। ठीक इसके विपरीत, निम्न वर्ग के लोगों में निम्नता की भावना होने के कारण, वे उच्च वर्ग के लोगों से मिलने या संबंध बढ़ाने में झिझक महसूस करते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वर्ग व्यवस्था में भी जाति की तरह अन्य समूहों के साथ रखने एवं खाने-पीने पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। इसमें केवल अपने वर्ग के सदस्यों के साथ संपर्कों को प्राथमिकता दी जाती है।
- आर्थिक आधार-वर्ग निर्माण में आर्थिक आधार को ही प्रधानता दी जाती है। विशेषकर माक्र्स ने वर्ग निर्माण में आर्थिक आधार को प्रधानता दी है। सामान्यतः समाज तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त होता है—
- उच्च वर्ग,
- मध्यम वर्ग तथा
- निम्न वर्ग। इन वर्गों को पुनः
निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-
8.सामान्य जीवन-यद्यपि प्रत्येक वर्ग के सदस्य को किसी भी प्रकार के जीवन-यापन की स्वतंत्रता होती है। फिर भी, वर्ग के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि जिस प्रकार का वर्ग हो उसकी के अनुरूप सदस्य जीवन-यापन करें। उच्च,मध्यम एवं निम्न, तीनों वर्गों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट जीवन प्रतिमान होता है और उससे संबंधित सदस्य उसे अपनाते हैं। इतना ही नहीं, एक वर्ग के सदस्यों के जीवन अवसरों में भी समानता पायी जाती है।
9.सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण–वर्ग सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारण करता है। व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होता है उसी के अनुरूप समाज में उसकी प्रस्थिति निर्धारित हो जाती है। पंतु यह प्रस्थिति स्थायी नहीं होती है, क्योंकि मुक्त व्यवस्था होने के कारण स्वयं वर्ग की सदस्यता व्यक्ति की योग्यता के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
प्रश्न 8.
जाति किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
या
जाति को परिभाषित कीजिए तथा वर्ग से इसका अंतर बताइए।
या
जाति से आप समझते हैं? इसे बंद वर्ग क्यों कहा जाता है? विवेचना कीजिए।
उत्तर-
भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की एक अनुपम व्यवस्था पायी जाती है जिसे जाति प्रथा कहते हैं। जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है तथा वह संपूर्ण जीवन उसी का सदस्य बना रहता है अर्थात् जाति की सदस्यता को किसी भी कार्य से बदला नहीं जा सकता। इसीलिए इसे सामाजिक स्तरीकरण की बंद व्यवस्था भी कहा जाता है। जातियों की सामाजिक स्थिति में काफी अंतर पाया जाता है अर्थात् इनमें संस्तरण पाया जाता है।
जाति का अर्थ एवं परिभाषाएँ
समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म लेने के स्थान व समुह से निर्धारित होती है। जाति भी व्यक्तियों का एक समूह है। जाति कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमानों को मानने वाला वह समूह है जिसके सदस्यों में रक्त शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है, जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। और जन्म भर उस सदस्यता का त्याग नहीं करता है। इस प्रकार का समूह सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है। इस समूह के सदस्य अन्य किसी समूह के सदस्य नहीं होते हैं और न किसी बाहर के समूह के सदस्य इस समूह के सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार जाति एक बंद वर्ग है।
‘जाति’ शब्द अंग्रेजी के ‘कास्ट’ (Caste) शब्द का हिंदी अनुवाद है जो पुर्तगाली भाषा के ‘कास्टा’ (casta) शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है ‘नस्ल’, ‘प्रजाति’ या ‘भेद’। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में गार्सिया दी ओरटा (Garcia de Orta) ने किया था। विद्वानों ने जाति की परिभाषा भिन्न-भिन्न आधारों पर की है। प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-
चार्ल्स कूल (Charles Cooley) के अनुसार-जब एक वर्ग आनुवंशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं।”
हॉबेल (Hoebel) के अनुसार-“अंतर्विवाह तथा आनुवंशिकता द्वारा थोपे हुए पदों को जन्म देना ही जाति व्यवस्था है।”
मैकाइवर एवं पेज (Maclver and Page) के अनुसार-“जब सामाजिक पद पूर्णत: निश्चित हो, जो जन्म से ही मनुष्य के भाग्य को निश्चित कर दे, जीवन-पर्यंत उसके परिवर्तन की कोई आशा न हो, तब वह जन वर्ग जाति का रूप धारण कर लेते हैं।”
केतकर (Ketkar) के अनुसार-“जाति की सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जो उसी जाति में जन्म लेते हैं तथा एक कठोर सामाजिक नियम अपनी जाति के बाहर विवाह करने से रोकता है।”
दत्त (Dutta) के अनुसार-“एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। …….. अनेक जातियों में कुछ निश्चित व्यवसाय हैं। …………. मनुष्य की जाति का निर्णय जन्म से होता है।”
ऊपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति व्यक्तियों का एक अंतर्विवाही समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, एक परंपरागत व्यवसाय होता है, जिसके सदस्य एक ही स्रोत से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं तथा काफी सीमा तक सजातीयता का प्रदर्शन करते हैं।
जाति की प्रमुख विशेषताएँ
जाति के प्रमुख लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है-
1. भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन-जाति व्यवस्था से भारतीय समाज खंडों में विभाजित हो गया है और यह विभाजन सूक्ष्म रूप में हुआ है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति तथा भूमिका सुस्पष्ट व सुनिश्चित रूप से परिभाषित हुई है। घुरिये ने इसे सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता माना है। उनके शब्दों में, “इसका तात्पर्य यह है कि जाति व्यवस्था द्वारा बँधे समाज में हमारी भावना भी सीमित होती है, सामुदायिक भावना संपूर्ण मनुष्य समाज के प्रति न होकर केवल जाति के सदस्यों तक सीमित होती है तथा जातिगत आधार पर सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार, यह विभाजन एक नैतिक नियम है और प्रत्येक सदस्य इसके प्रति सचेत होता है। यह उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराता है जिसके आधार पर वे अपने पद और कार्यों में दृढ़ होते हैं। साधारणतः कर्तव्य-पालन न करने पर जाति से निष्कासन की व्यवस्था होती है। या आर्थिक दंड दिया जाता है।
2. ऊँच-नीच की परंपरा अथवा संस्तरण-जाति व्यवस्था में ऊँच-नीच की परंपरा मान्य होती है जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता है और निम्न स्तर शूद्र लोगों का होता है। क्षत्रिय व वैश्य लोगों की स्थिति क्रमशः इसके मध्य की होती है। पुन: ये चार वर्ण अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हो गए हैं। हम की भावना सीमित होने से सदस्य केवल अपने वर्ण या जाति के लोगों को ही महत्त्व देते हैं और उनमें श्रेष्ठता की भावना भी जन्म लेती है। परंतु कुछ ऐसी भी जातियाँ हैं जिनमें सामाजिक दूरी इतनी कम है कि उनमें ऊँच-नीच के आधार पर जो सामाजिक संरचना स्पष्ट हुई है वही संस्तरण परंपरा है। जातीय संस्तरण रक्त की पवित्रता, पूर्वजों के व्यवसाय के प्रति आस्था व अन्यों के साथ भोजन व पानी के प्रतिबंध आदि विचारों पर आधारित होती है।
3. जन्म से जाति का निर्धारण-जाति व्यवस्था का निश्चय जन्म के साथ ही हो जाता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति समूह में वह जीवनपर्यंत रहता है। इस निश्चय, को न तो धनाढ्यता बदल सकती है, न निर्धनता, न सफलता और न असफलता ही। जाति के ही वंशधर उस जाति के सदस्य माने जाते हैं। जाति से बहिष्कार द्वारा ही व्यक्ति निम्न जाति में जाता है,अन्य किसी भी कारक द्वारा व्यक्ति अपनी जाति की सदस्यता परिवर्तित नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में ए०आर० वाडिया ने कहा है-“हिन्दू जन्म से ही हिंदू हो सकता है। रूढ़िवादी जाति व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति परिवर्तन के द्वारा हिंदू नहीं हो सकता है।”
4. भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध-भारतीय जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए अपने समूह के बाहर भोजन और सामाजिक सहवास पर नियंत्रण रखती है। इन नियमों का बड़ी कठोरता से पालन किया जाता है। नगरीकरण और आवागमन के साधनों के विकास के कारण अब यह नियंत्रण नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ढीला होता जा रहा है, पर गाँवों में यह नियंत्रण आज भी काफी मात्रा में देखा जा सकता है। प्रत्येक जाति में ऐसे नियम बड़े सूक्ष्म रूप से बनाए गए हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी जाति के सदस्य को (मुख्यतः जो ऊँची जातियों के हैं) कहाँ कच्चा भोजन करना है, कहाँ पक्का तथा कहाँ केवल जल ग्रहण करना है और कहाँ जल पीना भी निषिद्ध है। आधुनिक युग में यातायात के साधनों व शिक्षा में विकास के कारण और शासकीय प्रयत्नों आदि के कारण ये निषेध कमजोर होते जा रहे हैं। फिर भी, ग्रामीण भारत में आज की परिस्थिति में काफी हद तक ये सीमाएँ या निषेध प्रचलित हैं।
5. अंतर्विवाह–सभी जातियाँ अंतर्विवाही होती हैं अर्थात् जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है। यह निषेध आज बहुत जगहों में जाति तक नहीं वरन् उपजाति तक सीमित हो गया है। जाति व्यवस्था के अनुसार अंतर्जातीय विवाह अस्वीकृत हैं। वेस्टरमार्क (Westermarck) ने जाति व्यवस्था की इस विशेषता को इसका सार-तत्त्व माना है। घुरिये (Ghurye) का भी यही मत है कि जाति व्यवस्था का अंतर्विवाही सिद्धांत इतना कठोर है कि समाजशास्त्री इसे जाति व्यवस्था का प्रमुख तत्त्व मानते हैं। व्यावहारिक रूप में यह अंतर्विवाह भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बँधा हुआ है। एक जाति की कई उपजातियाँ होती हैं और प्रायः एक ही प्रांत में रहने वाली उपजातियों में विवाह होते हैं।
6. परंपरागत पेशों का चुनाव-मुख्यतः सभी जातियों के कुछ निश्चित पेशे होते हैं और जाति के सदस्य अपने उन्हीं पैतृक पेशों को स्वीकार करते हैं। उन्हें छोड़ना उचित नहीं समझा जाता। जाति का परंपरागत पेशा; चाहे वह व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करे या न करे, उसे मानसिक संतोष हो या न हो; व्यक्ति को ही अपनाना पड़ता है। साधारणतः लोग अपने पैतृक पेशे को ही अपनाना उचित समझते रहे हैं। पेशों का भी निर्धारण ऊँच-नीच के आधार पर होता रहा है। यदि उच्च जाति को कोई व्यक्ति निम्न जाति के पेशों को अपमाता था तो उनका जातीय विरोध होता था। इसी प्रकार, निम्न जाति का सदस्य जब उच्च जाति के पेशों को अपनाता था तो उसका भी विरोध होता था। परंतु आजकल इन नियमों में भी शिथिलता आ गई है।
7. धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताएँ एवं विशेषाधिकार—जिस प्रकार जाति व्यवस्था में संस्तरण है ठीक उसी प्रकार इसमें धर्म और समाज संबंधी निर्योग्यताएँ भी हैं। प्रत्येक मानव निवास की जगह में, मुख्यतः गाँवों में, यदि देखा जाए तो अछूतों और अन्य निम्न जातियों की निवास व्यवस्था गाँव के छोर पर रहती थी। उनके धार्मिक और नागरिक अधिकार भी सीमित होते थे। इसके विपरीत, ऊँची जातियों को सभी अधिकार प्राप्त रहे हैं तथा धर्म की पूरी छूट थी। साधारणत: शारीरिक श्रम करने वाली जातियाँ निम्न समझी जाती रही हैं। त्रावनकोर के वैकर्म (Vaikam) गाँव की विशिष्ट गलियों में अछूत जातियों ने प्रवेश करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। परंपरागत रूप से दक्षिण भारत में तो ये निर्योग्यताएँ अपनी चरम सीमा पर रही हैं। वहाँ अछूतों को कुछ विशेष सड़कों पर चलने की मनाही थी। इतिहास इस बात का उदाहरण है कि पेशवाओं और मराठों ने पूना शहर के दरवाजों के भीतर मसार और मूंग जाति के लोगों का शाम तीन बजे से सुबह नौ बजे तक प्रवेश वर्जित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत में अछूत सवर्णो के ऊपर अपनी छाया नहीं डाल सकते थे तथा उनके सामने नहीं जा सकते थे। ब्लेंट (Blunt) ने कहा कि गुजरात में दलित जातियाँ अपने विशिष्ट चिह्न के रूप में सींग पहना करती थीं।
8. आर्थिक असमानता-जाति व्यवस्था में आर्थिक असमानता का भी समावेश है। जाति व्यवस्था के निर्माण के साथ-साथ यह भावना भी चली कि जो निम्न है उसे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। निम्न जाति के कार्य, चाहे वह जीवन-यापन के लिए कितने ही उपयोगी क्यों न हों, मूल्यों की दृष्टि से हीन समझे जाते रहे हैं। इस प्रकार उनकी आय, संपत्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों भी बहुत कम रही हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा आदि का सदा से अभाव रहा है। परंपरागत रूप से भारतीय जाति व्यवस्था की यह विशेषता रही है कि सामान्यतः उच्च जातियों की आर्थिक स्थिति भी उच्च रही है और निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति भी निम्न रही है।
जाति एवं वर्ग में अंतर
जाति एवं वर्ग में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं-
- स्थायत्वि में अंतर-वर्ग में सामाजिक बंधन स्थायी व स्थिर नहीं रहते हैं। कोई भी सदस्य अपनी योग्यता से वर्ग की सदस्यता परिवर्तित कर सकता है। जाति में सामाजिक बंधन अपेक्षाकृत स्थायी व स्थिर रहते हैं। जाति की सदस्यता किसी भी आधार पर बदली नहीं जा सकती है।
- सामाजिक दूरी में अंतर-वर्ग में अपेक्षाकृत सामाजिक दूरी कम पायी जाती है। कम दूरी के कारण ही विभिन्न वर्गों में खान-पान इत्यादि पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं पाए जाते हैं। विभिन्न जातियों में, विशेष रूप से उच्च एवं निम्न जातियों में अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक दूरी पायी जाती है। इस सामाजिक दूरी को बनाए रखने हेतु प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर अन्य जातियों के सदस्यों के साथ खान-पान, रहन-सहन इत्यादि के प्रतिबंध लगाती है।
- स्वतंत्रता की मात्रा में अंतर-वर्ग में व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता रहती है। इसीलिए वर्ग को ‘खुली व्यवस्था’ भी कहा जाता है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति पर खान-पान, विवाह आदि से संबंधित अपेक्षाकृत कहीं अधिक बंधन होते हैं। जाति इन्हीं बंधनों के कारण ‘बंद व्यवस्था’ कही जाती है।
- प्रकृति में अंतर-वर्ग में मुक्त संस्तरण होता है अर्थात् व्यक्ति वर्ग परिवर्तन कर सकता है। जाति में बंद संस्तरण होता है अर्थात् जाति का परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- सदस्यता में अंतर-वर्ग की सदस्यता व्यक्तिगत योग्यता, जीवन के स्तर एवं हैसियत आदि पर आधारित होती है। जाति की सदस्यता जन्म से ही निश्चित हो जाती है।
- चेतना में अंतर-वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना रहती है। जाति के सदस्यों में यद्यपि अपनी जाति के प्रति चेतना तो पायी जाती है परंतु किसी. प्रतीक के प्रति चेतना की आवश्यक
- राजनीतिक अंतर-वर्ग की व्यवस्था प्रजातंत्र में अपेक्षाकृत अधिक, बाधक नहीं है। जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में अपेक्षाकृत बाधक है। जाति असमानता पर आधारित है, जबकि प्रजातंत्र समानता के मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है।
- व्यावसायिक आधार पर अंतर-वर्गों में परंपरागत व्यवसाय पर जोर नहीं दिया जाता और न ही विभिन्न वर्ग परंपरागत व्यवसायों से संबंधित हैं। इसके विपरीत, जाति में परंपरागत व्यवसाय पर विशेष जोर दिया जाता है। परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था। यह व्यवसाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था और इसे बदलना सरल नहीं था।
- संस्तरण में अंतर-वर्ग में मुक्त संस्तरण में होता है अर्थात् व्यक्ति अपना वर्ग परिवर्तित करे सकता है। इसके विपरीत, जाति एक बंद संस्तरण है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जीवन भर उसे उसी जाति का सदस्य बनकर रहना पड़ता है।
निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ग पश्चिमी समाज में पायी जाने वाली ऊँच-नीच की व्यवस्था है जिसमें अपेक्षाकृत खुलोपन पाया जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जाति एक बंद व्यवस्था है, जबकि वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति एक बंद व्यवस्था इसलिए है। क्योंकि इसकी सदस्यता बदली नहीं जा सकती है। वर्ग इसलिए खुली व्यवस्था है क्योंकि इसकी सदस्यता बदली जा सकती है। यदि वर्ग में भी जाति जैसे बंधन लग जाएँ तो यह एक जाति बन जाएगा। इसलिए मजूमदार का यह कहना है कि “जाति एक बंद वर्ग है” पूर्णतया सही है।
प्रश्न 9.
प्रजाति किसे कहते हैं? प्रजाति की विशेषताएँ बताइए।
या
प्रजाति किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण को एक स्वरूप है? समझाइए।
या
भारत को प्रजातियों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? विवचेना कीजिए।
उत्तर-
प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। यह मानवों के उस समूह को प्रकट करती है जिसमें शारीरिक व मानसिक लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। शरीर के रंग, खोपड़ी और नासिका की बनावट व अन्य अंगों की बनावट के आधार पर विभिन्न प्रजाति समूहों को देखते ही पहचाना जा सकता है। प्रजातीय दृष्टि से भी भारतीय समाज अनेक वर्गों में विभक्त हो गया है। भारतवर्ष में संसार की सभी प्रमुख प्रजातियों की विशेषताओं वाले लोग पाए जाते हैं। आदिकाल से ही भारत विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थल रही है। तभी से सभी का अपना अलग-अलग अस्तित्व भी रही है। शारीरिक दृष्टि से विभिन्न प्रजातियाँ परस्पर एक-दूसरे से अलग-अलग रही हैं, परंतु सभी लोग एक-दूसरे का अस्तित्व मानते रहे हैं और अमेरिका आदि की तरह यहाँ कभी भी रंगभेद पर आधारित प्रजातीय संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि यह सच है कि आज प्रजातिवाद की समस्या भारत के सामने नहीं है परंतु प्राचीन समय से लेकर आज तक मनुष्य का रंग अर्थात् वर्ण एक सामाजिक महत्त्व का विषय रहा है। वैदिक काल में द्रास, दस्यु, असुर, राक्षस सभी काले वर्ण के थे जबकि देवता, आर्य, श्रेष्ठजन सभी गौर वर्ण के थे। आज भी वैवाहिके विज्ञापनों में गौरवर्ण वधू की माँग की जाती है। गोरा रंग सौंदर्य, शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है।
प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषाएँ
प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। ‘प्रजाति’ शब्द का प्रयोग सामान्यत: उस वर्ग के लिए किया जाता है। जिसके अंदर सामान्य गुण हैं अथवा कुछ गुणों द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पायी जाती है। प्रमुख विद्वानों ने प्रजाति की परिभाषा निम्न प्रकार से की है–
हॉबेल (Hoeble) के अनुसार-“प्रजाति एक प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि शारीरिक विशेषताओं का विशिष्ट योग धारण करता है।”
रेमंड फिर्थ (Raymond Firth) के अनुसार-“प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके कुछ, वंशानुक्रमण द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण होते हैं।”
क्रोबर (Kroeber) के अनुसार-“प्रजाति एक प्रमाणित प्राणिशास्त्रीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो कि वंशानुक्रमण, नस्ल या प्रजातीय गुणों या उपजातियों के द्वारा जुड़ा है।”
बेनेडिक्ट (Benedict) के अनुसार–“प्रजाति पैतृकता द्वारा प्राप्त लक्षणों पर आधारित एक वर्गीकरण है।” उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है।
प्रजाति की विशेषताएँ
विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर प्रजाति की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं-
- प्रजाति का अर्थ जन-समूह से होता है। अतः इसमें पशुओं की नस्लों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- इस मानव समूह से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों से नहीं है वरन् प्रजाति में मनुष्यों का वृहत् संख्या में होना अनिवार्य है।
- इस मानव समूह में एक समान शारीरिक लक्षणों का होना अनिवार्य है। ये लक्षण वंशानुक्रमण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर इन्हें दूसरी प्रजातियों से पृथक् किया जाता है।
- प्रजातीय विशेषताएँ प्रजातीय शुद्धता की स्थिति में अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं अर्थात् भौगोलिक पर्यावरण के बदलने से भी किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण नहीं बदलते हैं।
प्रजाति के तत्त्व
प्रजाति कुछ विशेष तत्त्वों से मिलकर बनती है। यह विशेष तत्त्व उसके अस्तित्व को दूसरी प्रजातियों से भिन्न करते हैं। इन विशेष तत्त्वों के आधार पर ही प्रजाति का वर्गीकरण होता है। सामान्य रूप से प्रजातियों में तीन प्रकार के तत्त्व पाए जाते हैं-
- अंतर्नस्ल के तत्त्व-एक प्रजाति के लोग दूसरी प्रजाति के लोगों से विवाह नहीं करते हैं। इसका कारण पहले काफी सीमा तक भौगोलिक स्थिति रहा है। भौगोलिक स्थितियों के कारण एक प्रजाति के लोग दूसरों से कम मिल पाते हैं। दूसरे प्रत्येक प्रजाति स्थायित्व रखने का प्रयत्न करती है। गतिशीलता के अभाव में अंतर्नस्ल का तत्त्व (Elements of inbreeding) उग्र रूप से पाया जाता है; जैसे–टुंड्रा प्रदेश के लैप, सेमीयड और एस्कीमी मानव। इनमें अंतर्रजातीय विवाह होता है। यही कारण है कि इनमें अंतर्नस्ल के तत्त्व उग्र रूप से मिलते हैं। इस प्रकार के विवाह से रक्त की शुद्धता, संस्कृति की रक्षा तथा समान प्रजातीय लक्षणों को स्थायित्व होता है। ऊँची प्रजातियाँ भी अपनी रक्त की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतर्रजातीय विवाह करती हैं।
- विशेष शारीरिक लक्षणों के तत्त्व-प्रजातियों का वर्गीकरण शारीरिक लक्षणों के आधार पर भी किया जाता है। प्रत्येक प्रजाति में कुछ विशेष शारीरिक लक्षण (Distinctive physical traits) पाए जाते हैं; जैसे-शरीर का रंग, बाल, आँख, खोपड़ी, नासिका, कद, जबड़ों की बनावट आदि। वर्तमान समय में यातायात के साधनों में वृद्धि होने से शारीरिक लक्षण धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं।
- वंशानुक्रमण के लक्षणों के तत्त्व-प्रजाति का तीसरा तत्त्व वंशानुक्रमण के लक्षणों (Inheritance of traits) से संबंधित है। मेंडल के सिद्धांत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सहवास से रक्त में उन्हीं लक्षणों का अस्तित्व होता है जो पैतृक होते हैं या वंश परंपरा से चले आ रहे होते हैं। शारीरिक लक्षण एक श्रृंखला के समान होते हैं जो वंश परंपरा के कारण अनेक पीढ़ियों तक चलते हैं, जैसे कि नीग्रो का पुत्र नीग्रो ही होता है। वह कभी भी श्वेत प्रजाति के लक्षणों से युक्त नहीं होता है। प्रजाति की पवित्रता और संस्कृति की रक्षा पैतृक गुणों के द्वारा ही। होती है।
भारत में प्रजाति विविधता
भारत एक प्राचीन देश है। जब आर्य प्रजाति के लोग भारत में आए तो द्रविड़ प्रजाति के लोग पहले से ही अनेक आधारों पर ऊँच-नीच की श्रेणियों में बँटे हुए थे। समय-समय पर भारत में अनेक प्रजातियों के लोग आए और यहीं पर बस गए। इन सभी प्रजातियों के पारस्परिक मिलन व मिश्रण से अनेक नवीन प्रजातियाँ विकसित हुईं तथा साथ ही इस मिश्रण के कारण विशुद्ध प्रजातीय लक्षणों के स्थान पर मिश्रित लक्षण महत्त्वपूर्ण होते गए। आज भारत में विश्व की सभी प्रमुख प्रजातियों के लोग निवास करते हैं तथा इसीलिए उचित ही भारतवर्ष को प्रजातियों को अजायबघर कहा गया है। भारत में निवास करने वाली प्रमुख प्रजातियाँ निम्नांकित हैं-
- द्रविडयन-द्रविड़ या द्रविडयन (Dravidians) भारत की अत्यंत प्राचीन प्रजाति है। इस प्रजाति के लोग गंगा नदी के निचले हिस्सों में पाए जाते हैं। चेन्नई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और नागपुर में इस प्रजाति के लोग अधिक पाए जाते हैं। ये लोग कद में छोटे, बाल सामान्य व लहरदार, रंग काला, भारी चौड़ी नाक, काली तथा गहरी आँखें और लंबे सिर वाले होते हैं।
- इंडो-आर्यन-पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडो-आर्यन . (Indo-Aryans) प्रजाति के लोग अधिकतर देखे जा सकते हैं। इनके सदस्य लंबे कद, गोरे और गेहुँए रंग, लंबे सिर, पतली और लंबी नाक तथा काली आँखों वाले होते हैं। इन लोगों के शरीर पर काले और घने बाल भी पाए जाते हैं।
- मंगोलॉयड-मंगोलॉयड (Mangoloid) प्रजाति के लोग संपूर्ण भारत में काफी अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। हिमालय की तलहटी, हिमालय प्रदेश, बिहार और असम के उत्तरी सीमा प्रांत में ये लोग निवास करते हैं। ये लोग चौड़े सिर, औसत कद, कुछ पीला रंग, गोल चेहरा, शरीर पर बाल, भारी और अधखुली आँखें आदि शारीरिक विशेषताएँ लिये होते हैं। इन लोगों की नाक चपटी होती है।
- आर्यों-द्रविडयन-आय-द्रविडियन (Aryo-Dravidians) प्रजाति के लोग आर्य और द्रविड़ प्रजाति के मिश्रण का प्रतिफल हैं तथा राजस्थान, बिहार, दक्षिण-पश्चिम, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पंजाब के क्षेत्रों में ये लोग फैले हुए हैं। इन लोगों का कद मध्यम होता है। गेहुंआ रंग अथवा साँवले रंग के ये लोग लंबी नाक और काले बालों वाले होते हैं।
- मंगोलो-द्रविडयन-मंगोलो-द्रविडयन (Mangolo-Dravidians) प्रजाति के लोग चौड़े सिर वाले होते हैं तथा सिर पीछे से कुछ चपटा होता है। इन लोगों का प्राय: काला रंग होता है। इनका कद मध्यम होता है, चेहरे पर घने बाल होते हैं तथा ये लोग पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अधिक पाए जाते हैं। विद्वानों का विचार है कि ये लोग मंगोल और द्रविड़ प्रजातियों के मिश्रण का परिणाम हैं।
- सीथो-द्रविडयन-सीथो-द्रविडियन (Scytho-Dravidians) प्रजाति के लोगों के संबंध में विद्वानों का विचार है कि ये लोग मध्य एशिया से भारत में आने वाली सिथियन प्रजाति और भारत के मूल निवासी द्रविड़ों की मिश्रित शाखा के हैं। कुर्ग, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में ये लोग अधिक फैले हुए हैं। प्राय: महाराष्ट्र के ब्राह्मण इस प्रजाति के प्रमुख प्रतिनिधि समझे जाते हैं। इनका रंग गोरा, सिर चौड़ा, मध्यम कद, नाक चौड़ी व सुंदर होती है। शरीर पर कम बाल होना इस प्रजाति के लोगों की विशेष शारीरिक विशेषता है।
- चौड़े सिर वाली प्रजाति–चौड़े सिरवाली (Brachycephalic) प्रजाति के ये लोग संपूर्ण । भारत में फैले हुए हैं। इनकी तीन उपशाखाएँ हैं-
- अल्पाइन (Alpine),
- डिनारिक (Dinaric) तथा
- आमनॉयड (Armonoid)।
अल्पाइन प्रजाति के लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है, कंधे चौड़े और नाक छोटी होती है। ये मध्यम कद के होते हैं। डिनारिक प्रजाति के लोग प्राय: आल्पस पर्वतमाला में रहते हैं। वे ढलवाँ माथे वाले होते हैं। इनकी उठी हुई ठोड़ी होती है, होंठ पतले होते हैं, गर्दन मोटी होती है, रंग काला होता है और सिर का पिछला भाग कुछ चपटापन लिए हुए होता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा दक्षिण भारत में ये लोग विशेष रूप से फैले हुए हैं। आर्मोनॉयड प्रजाति के लोग लगभग मंगोली-द्रविड़ियन प्रजाति की तरह होते हैं। मुंबई में ये लोग अधिकतर पाए जाते हैं।
निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहती हैं। प्रत्येक प्रजाति की संस्कृति दूसरी प्रजाति की संस्कृति से भिन्नता लिए हुए है। कुछ प्रजातियाँ एक-दूसरे के संसर्ग से बनी हैं। सभी भारतीय प्रजातियाँ सदियों से एक-दूसरे से मिलती रही हैं, परस्पर अपनी-अपनी संस्कृति लेती और देती रही हैं। इस प्रकार, किसी भी प्रजाति के संबंध में निश्चितता के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन-सी प्रजाति शुद्ध रह गई और कौन-सी प्रजाति अशुद्ध। हाँ, इतना अवश्य निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि भारतभूमि आदिकाल से विभिन्न प्रजातियों के अजायबघर या संग्रहालय के रूप में विद्यमान है।
प्रश्न 10.
सामाजिक स्तरीकरण में लिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
या
लैगिक असमता के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए।
या
भारत में लैगिक असमता के प्रमुख पहलू बनाइए।
उत्तर-
वर्तमान समय में लिंग असमता (लैंगिक असमता) संबंधी अध्ययन किसी एक राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सम्मिलित विषय नहीं रहा है, वरन् यह एक अंतर्राष्ट्रीय विषय हो गया है क्योंकि आधुनिक समय में विश्व का आकार लघु होता जा रहा है। वैश्वीकरण (Globalization) एवं उदारीकरण (Liberalization) की प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को एकबद्ध कर दिया है; अत: समाजशास्त्र जैसे विषय में लिंग संबंधी असमता एवं समस्याओं का अध्ययन और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यह विषय इस तथ्य पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष तथा स्त्री के मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं को तो स्वीकार किया जा सकता है, परंतु सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर पुरुष तथा स्त्री में भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा करना मानवता तथा मानव अधिकारों की धारणा के नितांत विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व में स्त्रियाँ यद्यपि विश्व जनसंख्या के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा संपूर्ण कार्य के दो-तिहाई भाग को पूरा करती हैं, परंतु इनके पास विश्व की संपत्ति का केवल दसवाँ भाग ही है। वर्तमान समय में विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित सद्-शासन (Good Governances) के सिद्धांत का संपूर्ण विश्व में जोरदार प्रचार तथा प्रसार किया जा रहा है। कानून का शासन लिंग पर आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। यह कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता के विचार का समर्थन करता है, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष।
लैगिक असमता का अर्थ
पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग एक जैवकीय तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक असमता’ कहा जाता है। लिंग (Gender) शब्द का प्रयोग पुरुषों तथा स्त्रियों के गुणों के कुलक तथा समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान इन्हीं अपेक्षाओं से होती है। ये अपेक्षाएँ इस विचार पर आधारित हैं कि कुछ गुण, व्यवहार, लक्षण, आवश्यकताएँ तथा भूमिकाएँ पुरुषों के लिए प्राकृतिक हैं, जबकि कुछ अन्य गुण एवं भूमिकाएँ स्त्रियों के लिए प्राकृतिक हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लिंग केवल जैवकीय तथ्य नहीं है क्योंकि लड़का या लड़की जन्म के समय यह नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या सोचना है अथवा किस प्रकार से प्रतिक्रिया करनी है। प्रत्येक समाज में पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग के रूप में उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएँ समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित की जाती हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा उन्हें उन सांस्कृतिक अपेक्षाओं का ज्ञान दिया जाता है जिनके अनुसार उन्हें व्यवहार करना है। ये सामाजिक भूमिकाएँ एवं अपेक्षाएँ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में अथवा एक ही समाज़ के विभिन्न युगों में भिन्न-भिन्न होती हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएँ एवं संस्थाएँ उन मूल्य व्यवस्थाओं एवं सांस्कृतिक नियमों द्वारा सुदृढ़ होती हैं जो स्त्रियों की हीन भावना की धारणा को प्रचारित करती हैं। प्रत्येक संस्कृति में अनेक प्रथाओं के ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जो स्त्रियों को दिए जाने वाले निम्न मूल्य स्थिति को परिलक्षित करते हैं। पितृसत्तात्मकता स्त्रियों को अनेक प्रकार से शक्तिहीन बना देती है। इनमें स्त्रियों के पुरुषों की तुलना में निम्न होने, उन्हें साधनों तक पहुँचने से रोकने तथा निर्णय लेने वाले पदों में सहभागिता को सीमित करने जैसी परिस्थितियाँ प्रमुख हैं। नियंत्रण के यह स्वरूप स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रखने में सहायता प्रदान करते हैं। स्त्रियों की अधीनता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति (जैसे उनके स्वास्थ्य, आय एवं शिक्षा का स्तर) तथा उनके पद अथवा स्वायत्तता एवं अपने जीवन पर नियंत्रण के अंश के रूप में देखी जा सकती है। इस प्रकार, लिंग असमान वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्त्व बन गया है। विश्व के अनेक समाजों में; विशेषकर विकासशील देशों में स्त्रियों के साथ समाज में प्रचलित विभिन्न कानूनों, रूढ़िगत नियमों के आधार पर विभेद किया जाता है तथा उनको पुरुषों के समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। स्त्री या फेमिनिस्ट विद्वानों के अनुसार लैंगिक असमता को स्त्री-पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री-पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
लैगिक असमता के प्रकार
प्रत्येक समाज में लैंगिक असमता अनेक रूपों में विद्यमान रहती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन (Amartya Sen) के अनुसार, लैंगिक असमता विश्व के-जापान से जांबिया, यूक्रेन से संयुक्त राज्य अमेरिका–सभी देशों में पायी जाती है, परंतु पुरुषों एवं स्त्रियों में असमता अनेक रूपों में होती है। यह एक सजातीय प्रघटना न होकर अनेक अंतर्संबंधित समस्याओं से जुड़ी प्रघटना है। इनके अनुसार लैंगिक असमता को सामान्यत: निम्नलिखित सात रूपों में देखा जा सकता है-
- मृत्यु दर में असमता–विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों एवं पुरुषों में असमता का एक प्रमुख प्रकार सामान्यता स्त्रियों की उच्च मृत्यु दर में परिलक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। मृत्यु असमती अत्यधिक मात्रा में उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया (चीन एवं दक्षिण एशिया सहित) में देखी जा सकती है।
- प्रासूतिक असमता-गर्भ में ही बच्चे के लिंग को ज्ञात करने संबंधी आधुनिक तकनीकी की उपलब्धता ने लैंगिक असमता के इस रूप को जन्म दिया है। लिंग परीक्षण द्वारा यह पता लगाकर कि होने वाला शिशु लड़की है, गर्भपात करा दिया जाता है। अनेक देशों में, विशेष रूप से पूर्व एशिया, चीन एवं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा ताईवान के अतिरिक्त भारत एवं दक्षिण एशिया में भी यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह उच्च तकनीक पर आधारित असमता है।
- मौलिक सुविधा असमता–मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक देशों में पुरुषों एवं स्त्रियों में असमता स्पष्टतया देखी जा सकती है। कुछ वर्ष पहले तक अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी थी। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों के साथ-साथ लैटिन अमेरिका में लड़कियों को लड़कों की तुलना में शिक्षा सुविधाएँ बहुत कम उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य मौलिक सुविधाओं के अभाव के कारण स्त्रियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाते हैं और न ही वे अनेक सामुदिायक कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकती हैं।
- विशेष अवसर असमता-यूरोप तथा अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित एवं अमीर देशों के साथ-साथ अधिकांश अन्य देशों में उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में लैंगिक पक्षपात स्पष्टतया देखा जा सकता है।
- व्यावसायिक असमता–व्यावसायिक असमता भी लगभग सभी समाजों में पायी जाती है। जापान जैसे देश में, जहाँ जनंसख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अन्य सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ पर भी रोजगार एवं व्यवसाय प्राप्त करना स्त्रियों के लिए पुरुषों की तुलना में काफी कठिन कार्य माना जाता है।
- स्वामित्व असमता-अनेक समाजों में संपत्ति पर स्वामित्व भी पुरुषों एवं स्त्रियों में असमान रूप से वितरित है। गृह एवं भूमि संबंधी स्वामित्व में भी स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई हैं। इसी के परिणामस्वरूप स्त्रियाँ वाणिज्यिक, आर्थिक तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं से वंचित रह जाती हैं।
- घरेलू असमता–परिवार अथवा घर के अंदर ही लैंगिक संबंधी में अनेक प्रकार की मौलिक असमानताएँ पायी जाती हैं। घर की संपूर्ण देखरेख से लेकर बच्चों के पालन-पोषण का पूरा दायित्व महिलाओं का होता है। अधिकांश देशों में पुरुष इन कार्यों में स्त्रियों की किसी प्रकार की सहायता नहीं करते हैं। पुरुषों का कार्य घर से बाहर काम करना माना जाता है। यह एक ऐसा श्रम-विभाजन है जो स्त्रियों को पुरुषों के अधीन कर देता है।
भारतीय समाज में लैगिक असमता के विभिन्न पहलू
प्रत्येक समाज में लैंगिक विषमता जीवन के लगभग सभी पहलुओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारतीय समाज के उपयुक्त उदाहरणों द्वारा लैंगिक असमान के विभिन्न पहलुओं को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-
1. सामाजिक पहलू-सर्वप्रथम लैंगिक असमता सामाजिक पहलुओं में परिलक्षित होती हैं। सामाजिक पहलुओं में पायी जाने वाली लैंगिक असमता समाजीकरण में लिंग भेदभाव, महिलाओं का यौन शोषण एवं उत्पीड़न, शिक्षा में पिछड़ापन, अज्ञानता एवं अंधविश्वास, कुपोषण, वैधव्य एवं विवाह-विच्छेद की समस्या तथा महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में देखा जा सकता है। महिलाओं के प्रति हिंसा परिवार के भीतर तथा परिवार से बाहर दोनों रूपों में देखी जा सकती है। महिलाओं के प्रति हिंसा का एक अन्य गंभीर रूप बालिका वध की समस्या के रूप में प्रचलित है। दक्षिण में आज भी अनेक बालिकाओं की जन्म लेने से पहले अथवा जन्म लेने के पश्चात् हत्या कर दी जाती है। दहेज न ला पाने के कारण महिलाओं पर होने वाला अत्याचार भी उनके प्रति हिंसा का ही प्रतीक माना जा सकता है। इस प्रकार, आज भी भारतीय महिलाएँ विविध प्रकार की हिंसा का शिकार हैं।
2. आर्थिक पहलू-रोजगार में भी महिलाएँ लैंगिक असमता के कारण पुरुषों से पिछड़ी हुई हैं। उदाहरणार्थ-परंपरागत रूप से भारतीय महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चहारदीवारी तक ही सीमित था। इसलिए उनके बाहर कार्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। केवल कुछ निम्न जातियों की महिलाएँ घर से बाहर कृषि कार्य अथवा अन्य घरेलू कार्य करती थीं। अंग्रेजी शासनकाल में महिलाओं में भी शिक्षा का प्रचलन हुआ तथा उन्हें घर से बाहर नौकरी करने के अवसर उपलब्ध हुए। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के रोजगार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, तथापि सभी प्रयासों के बावजूद आज भी भारतीय महिलाएँ रोजगार की समस्या का शिकार हैं। उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता है, मातृत्व के समय अवकाश एवं अन्य सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता है तथा कई बार वे अपने सेवायोजकों के द्वारा यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। असंगठित क्षेत्र में ठेकेदार, कारखानों के मालिक तथा सेवायोजक उनकी निर्धनता का नाजायज लाभ उठाते हैं तथा उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं।
3. राजनीतिक पहलू-लैंगिक असमता का परिणाम राजनीतिक पहलू में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राजनीतिक में महिलाओं को आगे आने के उतने अवसर उपलब्ध नहीं है जितने कि पुरुषों को हैं। अब जब भारतीय महिलाओं को हर प्रकार से पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा शिक्षा-प्रसार ने उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है तब ऐसी दशा में उन्हें राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने से रोकना कहाँ की बुद्धिमता है? स्वतंत्रता से पूर्व भी भारतीय महिलाएँ अपने पूर्ण तन-मन से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती थीं। भारतीय संविधान ने उन्हें हर प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए हैं तो उनका उपयोग करने की स्वतंत्रता देना भी आवश्यक है।
परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वह एक महिला माँ, पत्नी तथा बहू पहले है। और बाकी सब बाद में। उसका कर्तव्य सर्वप्रथम अपने पारिवारिक उत्तरदायत्वि को निभाना है। यदि वह अपने बाल-बच्चों की उपेक्षा करके राजनीतिक क्षेत्र में भाग लेती है तो वह अपने कर्तव्य-पथ से विमुख हो जाएगी। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के पश्चात् ही किसी महिला का राजनीति यो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करना अधिक उचित प्रतीत होता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लैंगिक असमता पर आधारित है तथा कार्य विभाजन के आधार पर महिलाओं को घर की चहारदीवारी तक ही सीमित रखना चाहता है।
महिलाओं की स्थिति में सुधार विविध प्रकार के कारण एवं सरकारी प्रयासों द्वारा संभव हो पाया है। अब जब भारतीय महिलाओं को हर प्रकार से पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। तथा शिक्षा-प्रसार ने उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है तब ऐसी दशा में उन्हें राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने से रोकना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? स्वतंत्रता से पूर्व भी भारतीय स्त्रियाँ अपने पूर्ण तन-मन से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेती थीं। भारतीय संविधान ने उन्हें हर प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए हैं तो उनका उपयोग करने की स्वतंत्रता देना भी आवश्यक है।
आज लैंगिक असमता के कारण ही भारत में राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान सुरिक्षत रखने संबंधी विधेयक बार-बार पेश किए जाने के बावजूद पारित नहीं हो पाया है। वैसे तो उनके लिए आधे स्थान सुरक्षित होने चाहिए परंतु अनेक राजनीतिक दल उन्हें एक-तिहाई स्थान देने में भी किसी-न-किसी कारण से आना-कानी कर रहे हैं।
एनसीईआरटी सोलूशन्स क्लास 11 समाजशास्त्र पीडीएफ
- 1. समाजशास्त्र एवं समाज
- 2. समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएँ एवं उनका उपयोग
- 3. सामाजिक संस्थाओं को समझना
- 4. संस्कृति तथा समाजीकरण
- 5. समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ
- 7. ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था
- 8. पर्यावरण और समाज
- 9. पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय
- 10. भारतीय समाजशास्त्री